Contents
दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध काल भक्तिकाल की भाषा, काव्य रूप और उस काल में प्रयुक्त छंदो के बारे में पढ़ने जा रहें है। यदि आप हिंदी विषय में नेट/जेआरएफ की तैयारी कर रहें है तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि भक्तिकाल से संबंधित सवाल हर बार परीक्षा में पूछे जाते है।
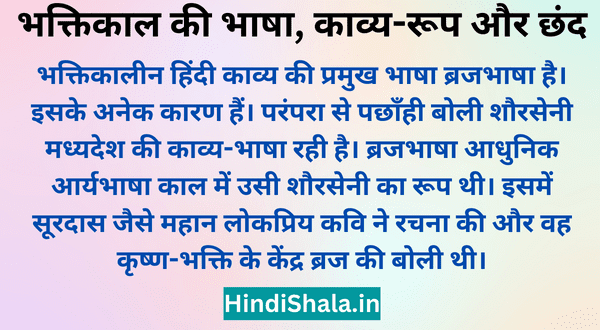
भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि
भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्यदेश की काव्य भाषा हिंदी-ब्रजभाषा का प्रचार-प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात् मराठी में और नानकदेव पंजाबी में रचना करते थे, तो वे ब्रजभाषा में भी रचनाएँ करते थे। चौदहवीं शती में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनीं, व्यापार की बढ़ोतरी हुई, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना-जुलना भी ज्यादा बढ़ा। इनमें सैनिक, व्यापारी तथा साधु-संत अधिक होते थे।
डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार– “पंद्रहवीं शती, सोलहवीं शती और सत्रहवीं शती में यहाँ व्यापार की बड़ी-बड़ी मंडियाँ कायम होती हैं, पचीसों नगर व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र बनकर उठ खड़े होते हैं।
लोहे और कपास का सामान काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। सैकड़ों वर्ष के बाद सामाजिक जीवन की धुरी गाँव से घूमकर नगर की ओर आ जाती है। इस समय सामाजिक जीवन की बागडोर सामंतों के साथ-साथ व्यापारियों के हाथ में आ जाती है, सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता है, समाचार भेजने के लिए हरकारों की व्यवस्था होती है। आज की भाषा में कहें तो एक प्रकार की दूरसंचार व्यवस्था कायम होती है। इससे मध्यदेश की भाषा के प्रचारित-प्रसारित होने की स्थिति तैयार होती है।
भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है। किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य में जायसी, रहीम और रसखान जैसे मुसलमान रचनाकारों का नाम नहीं सुनाई पड़ता। संभवतः भक्त कवियों की इतनी अधिक संख्या केवल हिंदी में है।”
भक्तिकाल की प्रमुख भाषा
भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाँही बोली शौरसेनी मध्यदेश की काव्य-भाषा रही है। ब्रजभाषा आधुनिक आर्यभाषा काल में उसी शौरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण-भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण-भक्ति की भाषा बन गई। भक्ति काव्य की ब्रजभाषा प्रवाह के कारण ब्रजभूमि के बाहर भी काव्य-भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। इसीलिए बाद में कहा गया कि “ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमान”।
इन्हें भी पढ़े :-
राम काव्यधारा की प्रवृतियाँ
कृष्ण काव्यधारा की प्रवृतियाँ
पूर्व-मध्यकालीन साहित्य में ब्रजभाषा एक प्रकार से भक्ति काव्य का पर्याय बन गई है। यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण और पूर्व के रचनाकारों ने भी ब्रजभाषा में रचना की। बंगाल- असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला-असमिया को ‘ब्रजबुलि’ कहा गया। भक्तिकाल की दूसरी भाषा अवधी है, यद्यपि यह ब्रजभाषा जितनी व्यापक नहीं। अवधी में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई है। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवधी में प्रबंध काव्य लिखे तो उसकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पैंगलम् के अनेक छंदों की भाषा अवधी कहीं-कहीं व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती है।
राहुल जी ने पउम चरिउ की भाषा में ‘कुंजी’ के शब्दों को अवधी कहा है। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से चौदहवीं और पंद्रहवीं शती में महत्त्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की जन्मभूमि अयोध्या के कारण तो वह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण था ही। खड़ी बोली में उस समय रचना अवश्य होती रही होगी जैसा कि अमीर खुसरो की कविताओं से प्रकट है, किंतु उसकी कोई परंपरा नहीं मिलती। भक्तिकाल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सधुक्कड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं-कहीं अवधी का भी पंचमेल है।
भक्ति साहित्य में प्रयुक्त छंद
भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, किंतु गेयपद और दोहा-चौपाई में निबद्ध कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना-रूप हैं। गेयपदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। नामदेव, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेयपदों में रचना की है। गेयपदों में काव्य और संगीत एक-दूसरे से घुल-मिल-से गए हैं। संभवतः ये कवि राग-रागिनियों को ध्यान में रखकर इन गेयपदों की रचना करते थे। गेयपदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती है अर्थात् वह केंद्रीय कथ्य होती है। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य की व्याख्या होती है और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेयपद समाप्त करता है।
वह अपने अनुभव से गेयपद के केंद्रीय कथ्य को सत्यापित करता है। दोहा – चौपाइयों की परंपरा भी सरहपा से मिलने लगती है, किंतु सरहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है, दोहा-चौपाइयों में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधी की प्रकृति अधिक अनुकूल है।
जायसी पूर्व अवधी कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध मिले हैं- जैसे भीम कवि का दंगव पुराण, सूरजदास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम का जैमिनि पुराण, ईश्वरदास की सत्यवती कथा आदि। किंतु यह रचना-रूप सूफ़ी कवियों, विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया।
दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। सरहपाद का दोहा-कोष प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला मारु रा दूहा जैसा प्रबंध काव्य भी मिलता है। भक्ति काव्य में कबीर के दोहे ‘साखी’ के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने रामकथा ‘दोहावली’ में रची। दोहे का ही एक रूप सोरठा है।
छप्पय, सवैया, कवित्त, भुजंग प्रयात, बावै, हरिगीतिका आदि भक्ति काव्य के बहुप्रयुक्त छंद हैं। सवैया, कवित्त हिंदी के अपने छंद हैं, जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं, जिनकी रचनाओं में मध्यकाल में प्रचलित प्रायः सभी काव्य-रूप मिल जाते हैं।
भक्तिकाल का काव्य रूप
तुलसी ने मंगलकाव्य, नहछू, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य-रूपों का भी उपयोग किया है। नहछू, कलेऊ विवाह के समय गाए जानेवाले और सोहर पुत्रजन्म के समय गाया जानेवाला गीत है।
आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए, पृथ्वीराज रासो में छंद बहुत जल्दी-जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी-जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी-जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं।
इस प्रकार, हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना-पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन बन गई। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्तिकाल इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। साहित्य में यह विविध विधाओं एवं कलात्मकता से युक्त होकर उत्कृष्ट रचनाओं के रूप में प्रकट हुआ।