Contents
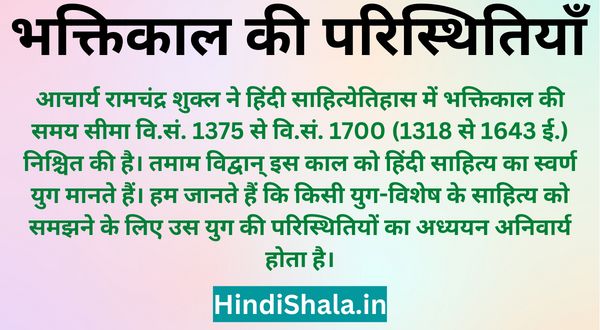
भक्तिकाल की परिस्थितियाँ
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्येतिहास में भक्तिकाल की समय सीमा वि.सं. 1375 से वि.सं. 1700 (1318 से 1643 ई.) निश्चित की है। तमाम विद्वान् इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हैं। हम जानते हैं कि किसी युग-विशेष के साहित्य को समझने के लिए उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन अनिवार्य होता है, क्योंकि युगीन परिस्थितियाँ साहित्य में प्रतिफलित होकर उसे अवश्यमेव प्रभावित करती हैं। भक्तिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं।
(क) राजनीतिक परिस्थितियाँ
राजनीतिक दृष्टि से भक्तिकाल का लगभग समय आतंक, अत्याचार, अशांति और संघर्ष का काल है। भक्ति-काल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक (सन् 1325 से 1351 ई.) के राज्य-काल से कुछ पूर्व हुआ और लगभग शाहजहाँ के राज्यकाल (सन् 1624 से 1658 ई.) के साथ इसका अंत हुआ। लगभग सातवीं शताब्दी में भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण का जो सिलसिला शुरू हुआ था, इस काल में भी वह जारी था। परिणामस्वरूप चौदहवीं शताब्दी के अंत तक प्रायः समूचे उत्तरी भारत पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था और यवन-सेनाएँ अब दक्षिण की ओर बढ़ने लगी थीं। 1
मुहम्मद गौरी के पश्चात् दिल्ली का शासन मुख्य रूप से क्रमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक और मुगल वंशों के हाथों में रहा। भारतीय नरेश पराजित अवश्य हो गए थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं की आपसी फूट के कारण अभी तक उन्होंने इस पराजित मनोवृत्ति को स्वीकार नहीं किया था और वे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। वस्तुतः मुगल सम्राट् बाबर के आक्रमण के पश्चात् ही यहाँ सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना हो सकी। इतिहास साक्षी है कि बाबर का सारा जीवन युद्धों में ही समाप्त हो गया। हुमायूँ और शेरशाह सूरी के शासनकाल भी राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वहीन ही माने जा सकते हैं। हाँ, अकबर ने अपने शासन-काल में भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और हिन्दू-मुसलमानों के मध्य बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता की खाई को पाटने का प्रयास किया। जहाँगीर और शाहजहाँ के शासन-काल में भी भारत में राजनीतिक शांति रही। परिणामस्वरूप अकबर से लेकर शाहजहाँ तक के काल में ही भक्ति-साहित्य को चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि भक्तिकाल के लगभग सारे प्रमुख कवि अपने देश के राजनीतिक वातावरण से अप्रभावित ही का प्रभाव ग्रहण नहीं किया। यों नानक और तलसी ने इस ओर संकेत किए हैं, लेकिन ये उनके मूल रहे हैं। कबीर, नानक, जायसी, तुलसी और सूरदास सरीखे प्रतिनिधि कवियों ने राजनीतिक वातावरण विषय कभी नहीं रहे। समग्रतः इन भक्तों की वाणी धर्म और शांति-प्रधान ही रही।
(ख) सामाजिक परिस्थितियाँ
चौदहवीं और पंद्रहवी शताब्दियों में हिन्दू-मुसलमानों में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, काफी आदान-प्रदान हुआ। इससे जहाँ पारस्परिक सद्भाव में वृद्धि हुई, वहीं जाति-पाति, खान-पान और विवाहादि के बंधन भी कठोरतर होते चले गए। कहीं-कहीं हिन्दू-मुसलमानों में विवाह संबंध भी स्थापित हुए। परिणामस्वरूप एक ही परिवार के कुछ लोग हिन्दू रह गए और कुछ मुसलमान बन गए। हिन्दुओं की बहू-बेटियों के अपहरण की बढ़ती घटनाओं का असर यह हुआ कि हिन्दू-समाज स्वयं को निरंतर संकुचित घेरे में बंद करता चला गया। बाल-विवाह, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति आदि कुरीतियाँ प्रचलित होकर सामाजिक व्यवस्था को क्षीण करने लगीं।
मुगलों ने शेरशाह सूरी द्वारा समाप्त की गई जमींदारी प्रथा को पुनः चालू कर दिया। इस प्रथा की छत्रछाया में पलने वाले जागीरदार, मनसबदार, रईस और जमींदार ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इसके विपरीत हिन्दू-समाज अभावों से ग्रस्त था। इतिहासकार बर्नीयर ने लिखा भी है कि “हिन्दुओं के पास धन-संचित करने के कोई साधन नहीं बचे थे और उनमें से अधिकतर को निर्धनता, अभावों एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्षरत जीवन व्यतीत करना पड़ता था। प्रजा के रहन-सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का सार भार उन्हीं पर था। राज्य-पद उनको अप्राप्त थे।”
डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने भक्तिकाल की सामाजिक परिस्थितियों के विषय में लिखा है-“समाज की छिन्न-भिन्न अवस्था तो पहले से ही चली आ रही थी; दूसरे, राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वह और भी अव्यवस्थित हो गई।” सामाजिक ढांचे की इस अवस्था को लक्ष्य करके ही कबीर और तुलसी को इस दिशा में अपना सुधारात्मक स्वर अधिक प्रबलता एवं वेग के साथ मुखरित करना पड़ा।
(ग) धार्मिक परिस्थितियाँ
राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश के अनुरूप ही धार्मिक परिवेश का होना स्वाभाविक था। भक्तिकाल के प्रारंभ में हिन्दू धर्म अनेक संप्रदायों और मत-मतांतरों में बुरी तरह विभक्त था। वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त, सिद्ध, नाथ और वाममर्गी एक-दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते थे। इसी समय इस्लाम का प्रभाव भी भारतीय धर्मों पर पड़ना शुरू हो गया था। शासक वर्ग हिन्दू धर्म पर अनेक प्रकार के अत्याचार करके उनके पवित्र ग्रंथों और पूजा-स्थलों को नष्ट करने पर तुला हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस ओर संकेत करते हुए लिखा था- “देश मलेच्छाक्रांत है। गंगा आदि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं। अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है।”
भक्तिकाल में उत्तर भारत में अनेक धार्मिक संप्रदायों- रामानन्दी संप्रदाय, संत संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय आदि का जन्म हुआ। इन संप्रदायों का जीवन, साहित्य तथा दार्शनिक विचारधारा सरल एवं सुगम था। सभी अपने-अपने दृष्टिकोण का प्रचार-प्रसार जनता की भाषा में कर रहे थे। जाति वर्ण-व्यवस्था आदि से संबंधित उनके विचार अत्यंत उदार थे। भक्ति और धर्म का मार्ग सबके लिए खुल चुका था। डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने भक्तिकाल को धार्मिक परिस्थितियों के विषय में लिखा है- “देश में ज्यों-ज्यों अराजकता कम होती गई, जीवन में स्थिरता आती गई, त्यों-त्यों धार्मिक आंदोलन भी अत्यंत तीव्रता के साथ समाज में अपना प्रभाव प्रकट करने लगे।”
धार्मिक दृष्टि से भक्तिकाल में दो मत-संत और भक्त प्रचारित हुए। निर्गुणवादियों को ‘संत’ तथा सगुणवादियों को ‘भक्त’ कहा गया। एक ओर निर्गुणी संतों और सूफियों ने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया, तो दूसरी ओर सगुणवादी रामभक्ति शाखा तथा कृष्णभक्ति शाखा ने मिलकर मानवीय धर्म को अधिक विस्तृत परिवेश प्रदान किया। अतः यह सहज ही कहा जा सकता है कि इस काल में जहाँ अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को प्रश्रय मिला, वहीं विशुद्ध मानवीय धर्म को भी बल मिलता प्राप्त हुआ।
(घ) सांस्कृतिक परिस्थितियाँ
भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है-समन्वय की चेष्टा भक्तिकाल 1 में निरंतर होने वाले बाह्य आक्रमणों का एक परिणाम यह भी हुआ कि बाह्य आक्रांता अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेते आए, जो कालांतर में भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बनती चली गई।
मध्यकालीन धर्म-साधना में प्रायः सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म-साधनाएँ किसी-न-किसी रूप में अवश्य पाई जाती हैं। इनमें शैव, शाक्त, भागवत और गाणपत्य धर्म-साधनाएँ उल्लेखनीय हैं। विभिन्न धर्मों अथवा संप्रदायों के बीच अनेक उपधर्मों का बनना मध्यकाल की मानो विशेषता ही बन गई थी। धार्मिक क्षेत्र में समन्वय-वृत्ति का अनुगूंज हमें तुलसी के “शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहिं पावा” में सहज ही सुनाई पड़ती है।
समन्वयात्मकता की यह प्रवृत्ति वास्तु एवं मूर्ति-कलाओं में भी लक्षित होती है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार, “एलोरा के समीपस्थ वेरूल के कैलाश-मंदिर में शिव की मूर्ति के शीर्ष स्थान पर बोधिवृक्ष स्थित है। चम्बा-नरेश अजयपाल के राज्यकाल में उत्कीर्ण ब्रह्मा, वरुण और शिव के साथ बुद्ध भी हैं। खजुराहो से उपलब्ध कोक्कल के वैद्यमान मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्मा, जिन, बुद्ध तथा वामन को शिव का स्वरूप कहा गया है। इसी प्रकार हरिहर-पूजन में भी शैव-वैष्णवधारा का संगम लक्षित होता है। संक्षेप में, ऐसे अनेक प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनसे समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है।”
हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों की निकटता के परिणामस्वरूप चित्र, संगीत और साहित्य-कलाओं में भी दोनों संस्कृतियों के उपकरणों का समावेश हुआ। इस काल के नायक-नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों में, भारतीय व ईरानी संगीत के सम्मिश्रण में तथा ‘आदिग्रंथ’ में प्राप्त राग-रागनियों और शैलियों में इस समन्वय की झलक प्राप्त होती है। इस वातावरण में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ।
(ङ) साहित्यिक परिस्थितियाँ
हम जानते हैं कि भाव, भाषा और उद्देश्य की सर्वोच्चता के कारण भक्तिकालीन हिन्दी-साहित्य सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया है। यद्यपि मुगलों ने फारसी को राजभाषा का सम्मान देकर संस्कृत और हिन्दी को गौण स्थान पर बिठा दिया था, तथापि तत्कालीन हिन्दी में भी लोकप्रिय साहित्य की रचना हुई। कबीर, जायसी, सूर और तुलसी के साहित्य के बल पर ही भक्तिकाल हिन्दी-साहित्य का स्वर्णयुग कहलाया है।
भक्तिकाल में संस्कृत में टीकाओं और व्याख्याओं की ही सृष्टि हुई-किसी मौलिक उद्भावना का जन्म नहीं हुआ। फारसी में अनेक इतिहास-ग्रंथों तथा प्रचुर मात्रा में काव्य का निर्माण हुआ। संस्कृत के अनेक धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का फारसी के माध्यम से अनुवाद भी सामने आया। राजस्थानी वचनिकाओं तथा ब्रजभाषा की वार्ताओं और टीकाओं में गद्य का प्रयोग भी प्रारंभ हो चुका था, लेकिन यह गद्य प्रारंभिक महत्त्व का ही रहा।
निःसंदेह इस काल में भक्ति-साहित्य ही रचा जाता रहा, साथ ही शासकों और राजाओं के दरबारों में प्रशस्ति, श्रृंगार, रीति, नीति आदि से संबंधित मुक्तक और प्रबंध-काव्यों की निर्मिति भी हुई। भक्तिकाल की यह गौण साहित्यिक प्रवृत्ति ही आगे चलकर ‘रीतिकाल’ में मुख्य हो गई।