Contents
- छायावाद का परिचय
- छायावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ
- 1. आत्माभिव्यक्ति
- 2. मानवीय सौन्दर्य का वर्णन छायावादी
- 3. प्रकृति का भव्य चित्रण
- 4. शृंगार- भावना
- 6. वेदना का निरूपण
- 7. मानवतावाद
- 8. राष्ट्रीय चेतना
- 9. दार्शनिकता
- 10. कल्पना शक्ति का प्रदर्शन
- 11. अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग
- 12. बिम्बात्मकता
- 13. प्रतीकात्मकता
- 14. परिनिष्ठित, परिमार्जित खड़ीबोली का प्रयोग
नमस्कार प्यारे दोस्तों ! आज के इस पोस्ट में हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे युग की चर्चा करने जा रहें है जिसे उसकी प्रवृत्तियों के कारण छायावाद का नाम दिया गया। इस युग में प्रमुख रूप से चार कवियों (सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत) को आधार स्तंभ माना गया है।
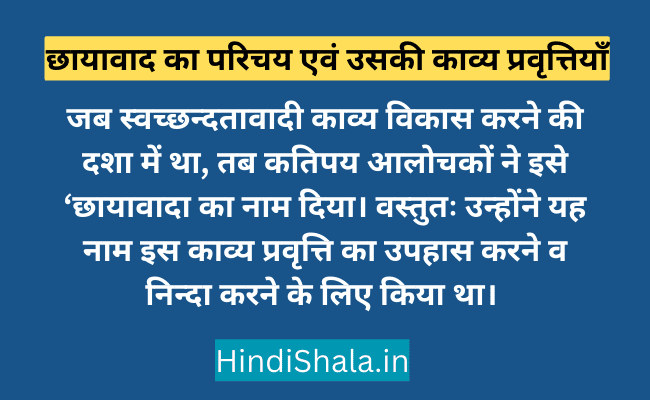
छायावाद का परिचय
जब स्वच्छन्दतावादी काव्य विकास करने की दशा में था, तब कतिपय आलोचकों ने इसे ‘छायावादा का नाम दिया। वस्तुतः उन्होंने यह नाम इस काव्य प्रवृत्ति का उपहास करने व निन्दा करने के लिए किया था। परन्तु स्वच्छन्दतावादी कवियों ने सजहता के साथ अपने काव्य के लिए प्रयुक्त इस शब्द को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार स्वच्छन्दतावादी काव्य के लिए ‘छायावादी काव्य’ शब्द का प्रयोग होने लगा। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पाण्डेय ने किया था।
“छायावाद’ शब्द को विद्वानों ने अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया है। इनमें से प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं-
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- “छायावादी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति के व्यापक अर्थ में है।”
डॉ० नगेन्द्र-“स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद का आधार है।”
जयशंकर प्रसाद – “छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं।
महादेवी वर्मा – “छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए सम्भव न हुआ, परन्तु उसकी सौन्दर्य स्थूल के आधार पर नहीं है–यह कहना स्थूल की परिभाषा को संकीर्ण कर देना है। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौन्दर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी।”
डॉ० रामकुमार वर्मा – “छायावाद वास्तव में हृदय की एक अनुभूति है। वह भौतिक संसार के क्रोड में प्रवेश कर अनन्त जीवन के तत्त्व ग्रहण करता है और उसे हमारे वास्तविक जीवन से जोड़कर हृदय में जीवन के प्रति एक गहरी संवेदना और आशावाद प्रदान करता है।”
छायावादी कवि छायावाद के चार स्तम्म माने जाते हैं-जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला,सुमित्रानंदन पन्त और महादेवी वर्मा। इनके अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, डॉ० रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मीनारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद ‘झाद्विज’ आदि को भी गणना छायावादी कवियों में होती है।
छायावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ
छायावादी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है:-
1. आत्माभिव्यक्ति
छायावादी कविता वस्तुतः द्विवेदी युगीन विषय-प्रधान कविता के विरोध में रची गई थी। फलतः इसमें कवियों ने अपने निजी सुख-दुःख से उत्पन्न अनुभूतियों को ही काव्य में निरूपित किया है। वही छायावादी कवियों-जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत व महादेवी वर्मा ने अपने हर्ष और विषाद की अनुभूति को काव्य में अभिव्यक्त किया है। इन कवियों के हृदय में अनुभूतियों का अक्षय भण्डार होता है और जब ये अनुभूतियाँ उसे विचलित करने लगती हैं, उसके मन को उद्वेलित करती हैं, तब उसके हृदय से जो वाणी निकलती है, वही कविता में प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिए चारों कवियों के काव्य में व्यक्त आत्माभिव्यक्ति देखिए-
जयशंकर प्रसाद
क्या कहूँ ? क्या हूँ मैं उद्भ्रांत
विवर में नील गगन के आज
वायु की भटकी एक तरंग
शून्यता का उजड़ा-सा राज।
सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला
मेरे अन्तर बज्र कठोर
देना जी भरसक झकझोर
मेरे दुख की गहन अन्यतम
निशि न कभी हो भोर
क्या होगी इतनी उज्ज्वलता
इतना वन्दन अभिनन्दन ?
जीवन चिरकालिक क्रन्दन ।
सुमित्रानन्दन पंत
हाय मेरे सामने ही प्रणय का,
ग्रन्थि बन्धन हो गया; वह नव-कुसुम
मधुप-सा मेरा हृदय लेकर, किसी-
अन्य मानस का विभूषण हो गया।
मैं नीर भरी दुःखी की बदली।
महादेवी वर्मा
मैं नीर भरी दुःखी की बदली।
स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कंदन में आहत विश्व हँसा।
नयनों में दीपक जलते, पलकों में निर्धारिणी मचली।
विस्तृत नम का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना।
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल की मिट आज चली।
2. मानवीय सौन्दर्य का वर्णन छायावादी
कवियों का मनुष्य ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ व सुन्दर कृति दि देती है। उन्होंने अपने काव्य में नर नारी व शिशु तीनों के आन्तरिक व बाहा सौन्दर्य का वर्णन किया है। पंत्र ने तो मनुष्य को इस संसार का सबसे सुन्दर प्राणी घोषित किया है-
सुन्दर हैं विहग सुमन सुन्दर,
मानव तुम सबसे सुन्दरतम ।
इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने मनुष्य विशेषकर नारी सौन्दर्य का बड़ी ही मनोरम वर्णन किया है। परन्तु उसमें अश्लीलता, अतिशयता का अभाव है। उन्होंने नारी सौन्दर्य का अत्यन्त उदात्त शैली में वर्णन किया है। उदाहरण के लिए वे ‘कामायनी’ में ‘श्रद्धा’ के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं-
नील परिधान बीच सुकुमार
खिल रहा मृदुत अपला अंग ।
खिला हो ज्यों बिजली का फूल
मेपवन बीच गुलाबी रंग ।
इसी प्रकार सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला ने भी अपने काव्य में मनुष्य-विशेषकर नारी के दोनों ही सौन्दर्य का वर्णन किया है। जहाँ तक महोदवी वर्मा के काव्य में मानवीय सौन्दर्य का प्रश्न है तो इस शारीरिक व अशारीरिक संबंध में यही कहा जा सकता है कि महादेवी ने मनुष्य के आन्तरिक अर्थात् भावपरक सौन्दर्य का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए-
उस असीम का सुन्दर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे।
मेरी श्वासें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्दन रे ।।
3. प्रकृति का भव्य चित्रण
छायावादी कवियों ने प्रकृति को विविध रूपों में चित्रित करके हिन्दी-साहित्य में प्रकृति-चित्रण की परम्परा को और अधिक सजीव सशक्त एवं समृद्ध किया है। विशेषकर कवि पंत तो सच्चे उपासक रहे हैं। वे प्रकृति के प्रतिपल बदलते देश को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। छायावादी कवियों ने अपने प्रकृति-चित्रण में प्रकृति के लगभग सभी परम्परागत रूपों यथा-आलम्बन रूप, उद्दीपन रूप संवेदनात्मक रूप, मानवीकरण रूप, वातावरण निर्माण रूप, रहस्यात्मक रूप, अलंकार-योजना रूप, प्रतीकाल रूप, लोक-शिक्षा रूप दूती के रूप में चित्रण किया है। इन कवियों में से कवि पंत ने तो प्रेमिका के सान्ति की तुलना में प्रकृति का आश्रय लेना बेहतर माना है-
छोड़ों की मृदु छाया
तोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले !तेरे बाल जाल में,
कैसे उलझा दूँ लोचन ।
जयशंकर प्रसाद ने ‘कामायनी में प्रकृति का मानवीकरण रूप में चित्रण करते हुए लिखा है-
अन्तरिक्ष में अभी सो रही ऊपा मधुवाला।
अरे खुली भी नहीं अभी तो प्राची की मधुशाला।
इसी प्रकार ‘बीती विभावरी जाग री’ कविता में तो उन्होंने प्रकृति-चित्रण में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। ‘लहर’ काव्य-संग्रह में संकलित इस कविता की कतिपय पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं जिनमें कवि ने प्रातः कालीन दृश्य का सजीव चित्रण किया है-
खगकुल कुल-कुल सा बोल रहा,
किसलय का आंचल डोल रहा
लो यह सतिका-सी भर लाई ।
मधु मुकुल नवल रस गागरी ।।
इसी प्रकार प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानन्दन पंत ने भी प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण किया है। उन्होंने आलम्बन रूप के दो भेदों-संश्लिष्ट चित्रण व नाम-परिगणन के अनुरूप ही प्रकृति का चित्रण किया है। यहाँ पर उनके द्वारा नाम परिगणन-प्रणाली व प्रकृति के प्रतीकात्मक रूप का चित्रण करने वाले दो उदाहरण प्रस्तुत हैं-
(क) नाम-परिगणन ( प्रकृति का आलम्बन रूप) –
महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली।
फूले आडू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली।
(ख) प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप-
द्रुत झरो जगत् के जीर्ण पत्र, हे ग्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण।
हिम ताप पीत, मपुवात भीत, तू वीतराग, जड़ पुराचीन।अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य में प्रकृति-चित्रण की प्रवृत्ति समान रूप से सभी कवियों में पाई जाती हैं। इस काव्य में प्रकृति का भव्य चित्रण हुआ है ।
4. शृंगार- भावना
भारतीय साहित्य में शृंगार के प्रति लगभग सभी कवियों ने विशेष रुचि दर्शाई है। छायावादी कवि भी इसका अपवाद नहीं हैं। छायावादी काव्य में शृंगार के उभय पक्षों का निरूपण हुआ है। इसमें कवियों ने शृंगार के संयोग-पक्ष, नारी के मांसल सौन्दर्य आदि का निरूपण किया है। उदाहरण के लिए, कवि निराला शेफालिका कविता में शारीरिक मांसल सौन्दर्य के अनुरूप ही प्रकृति का चित्रण किया है अर्थात् उन्होंने प्रकृति को नारी-रूप में दर्शाकर उसके स्थूल सौन्दर्य का इस प्रकार वर्णन किया है-
बन्द कंचुकी के सब खोल दिए प्यार से
यौवन उभार नेपल्लव पर्यंक पर सोती शेफालिके।
मूक आह्वान भरे-खासी कपोलों के
व्याकुल विकास पर
झरते हैं शिशिर से चुम्बन गगन के ।
अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य में श्रृंगारिक चेतना का दो रूपों-अतिसूक्ष्म स्थूल रूप में चित्रण हुआ है। स्थूल-श्रृंगार में कहीं-कहीं अश्लीलता व मांसलता का भी चित्रण हुआ है।
5. रहस्यवाद
छायावादी काव्य में उस अव्यक्त, अगोचर, असीम चेतन शक्ति के प्रति कवियों ने अ जो भावोद्गार व्यक्त किए हैं, उसे आलोचकों ने रहस्यवाद कहा है। आचार्य शुक्ल ने अनन्त, अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर कवियों की काव्याभिव्यक्ति को ही रहस्यवाद कहा है जबकि डॉ० रामकुमार वर्मा ने उसे जीवात्मा की उस अन्तर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन कहा है जिसे वह दिव्य व अलौकिक शक्ति से जोड़ने का प्रदान करती है। उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा उस असीम सत्ता के साथ अपना संबंध दर्शात हुए कहती हैं-
क्या पूजा क्या अर्चन रे!
उस असीम का सुन्दर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे!
मेरी श्वासें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्दन रे!
पदरज को धोने उमड़ आते लोचन में जलकण रे!
अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे!
6. वेदना का निरूपण
यद्यपि छायावादी कवियों ने सुख-दुख से उत्पन्न दोनों ही अनुभूतियों का अपने काव्य में चित्रण किया है परन्तु उन्होंने विरह वेदना का विशेष रूप से अपने काव्य में निरूपण किया है। पंत ने तो यह स्पष्ट ही कह दिया है कि पहला कवि कोई वियोगी ही हुआ होगा और उसका विरह ही कविता बनकर द प्रस्तुत हुआ होगा। इस प्रकार पंत कवि व कविता को वियोगी व विरह से जोड़कर देखते हैं; यथा-
वियोगी होगा पहला कवि,
आह से उपजा होगा गान
उमड़ कर आँखों से चुपचाप
बही होगी कविता अजान।
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य में चित्रित विरह-वेदना गांभीर्य से युक्त है, करुणा से ओतप्रोत है, उसमें नैसर्गिक भावों की सरिता बह रही है, उसमें विविध काम-दशाओं की कीड़ा भरी हुई है। इन कवियों को इस विरह-वेदना, पीड़ा में ही संयोग का सुख, हर्ष की सिरहन का आभास होता है।
7. मानवतावाद
छायावादी कवियों के मन में मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम है। वे जाति, धर्म देश की सीमाओं से ऊपर उठे हुए हैं। उनकी दृष्टि में विश्व के समस्त मानव समान हैं। यही कारण है कि मानवतावादी विचारों को अपनी कविता में निरूपित करते हैं। ‘कामायनी’ में जयशंकर प्रसाद अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखते हैं-
औरों को हँसते देखो मनु,
हँसो और सुख पाओ।
अपने सुख को विस्तृत कर तो
जग को सुखी बनाओ
अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य में प्रत्येक पुरुष, नारी, शिशु आदि के समुचित अधिकारों के लिए संदेश दिया गया है और उन्होंने जन-कल्याण, लोक-कल्याण व विश्व-कल्याण की भावना को दर्शाया है।
8. राष्ट्रीय चेतना
छायावादी कवियों ने अपने काव्य में अपनी राष्ट्रवादी भावना को भी अभिव्यक्त किया है। उनकी राष्ट्रीय चेतना कई रूपों में प्रकट होती है। एक ओर तो वे अपने देश के गौरवशाली अतीत का यशोगान करते हैं ताकि पराधीन भारतीय जनता में तो जातीय गौरव की भावना भरी जा सके; यथा- वही है रक्त वही है देशवही साहस है बैसा ज्ञान।वही है शान्ति, वही है शक्ति ,वही हम दिव्य- आर्य-संतान ।
जिएँ तो सदा इसी के लिए,
यही अभिमान रहे, यही हर्ष।
निछावर कर दें हम सर्वस्व,
हमारा प्यारा भारतवर्ष ।।
9. दार्शनिकता
छायावादी कवियों का भिन्न-भिन्न दर्शनों में विश्वास था। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। उनके महाकाव्य ‘कामायनी’ पर अनेक दर्शनों यथा प्रत्यभिज्ञा दर्शन, बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन आदि का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा का अधिकांश काव्य बौद्ध दर्शन पर आधारित है। निराला के काव्य पर अद्वैतवाद का तथा पंत के काव्य पर अरविन्द दर्शन, उपनिषदों, महात्मा गाँधी, विवेकानन्द जादि के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद ने शैव दर्शन से प्रभावित होकर अपने महाकाव्य ‘कामायनी’ में ‘आनन्दवाद’ की स्थापना की। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य में कवियों की दार्शनिक चेतना भी अभिव्यक्त हुई है।
10. कल्पना शक्ति का प्रदर्शन
छायावादी कवियों ने अपनी काव्य-रचनाओं में अपनी जिस कल्पना-शक्ति का परिचय दिया है, वह उनके काव्य को पूर्ववर्ती काव्य से बिल्कुल अलग कर देती है। छायावादी कवियों की नूतन कल्पना-शक्ति उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय देती है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में वर्ण्य विषय को एक नई कल्पना के साथ प्रस्तुत किया है फिर चाहे वह नारी सौन्दर्य का वर्णन हो, प्रकृति का वर्णन हो या आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति हो। उदाहरण के लिए कवि जयशंकर प्रसाद ‘कामायनी’ में श्रद्धा के रूप-सौन्दर्य व उसकी वेशभूषा का वर्णन करते समय अपनी मौलिक व नई कल्पना का परिचय देते हुए लिखते हैं-
नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अथला अंग ।
खिला हो ज्यों बिजली का फूल
मेघवन बीच गुलाबी रंग। पिर रहे ये घुंघराले बाल
अंस अवलम्बित मुख के पास।
नील-पन- शावक के सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास ।
11. अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग
छायावादी कवियों ने निस्संदेह अलंकारों का प्रयोग किया है परन्तु उसमें चमत्कार प्रदर्शन की भावना दिखाई नहीं देती है। इस काव्य में अलंकारों का सहज, स्वाभाविक व नैसर्गिक रूप से प्रयोग हुआ है। इन छायावादी कवियों में से पंत ने तो स्पष्ट ही कह दिया कि-
तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार।
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार।
12. बिम्बात्मकता
छायावादी काव्य में विम्बात्मकता का गुण भी देखने को मिलता है। ये बिम्ब कवि को अनुभूति, तीव्र भावना, उत्कृष्ट वासना से परिपूर्ण हैं तथा अपनी सजीवता, सुन्दरता आदि गुणों के लिए सजीव ने जान पड़ते हैं। इन बिम्बों अर्थात् शब्द-चित्रों के माध्यम से छायावादी कवियों ने अपनी कविता को चित्रमयी बना दिया है। छायावादी काव्य में ऐन्द्रिय बिम्ब, वस्तुपरक विम्ब, भाव विम्ब द दार्शनिक विम्ब का विधान है। यहाँ पर छायावादी काव्य में प्रयुक्त बिम्बों के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं-
(क) स्पृश्य-विम्य
नव वरांत के सरस स्पर्श से
पुलकित वसुधा बारम्बार ।
(ख) दृश्य-बिम्ब :
उन्माद यौवन के उभार,
घटा-सी नय असा की सुन्दर
अति श्याम वरण,
श्लय, मन्दर चरण ।
13. प्रतीकात्मकता
छायावादी कवियों ने ऐसे अनेक प्रतीकों का चुनाव किया है जो सूक्ष्म भावों, रूपविशेषों, व्यापारों आदि को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग से छायावादी काव्य में एक अपूर्व चमत्कार आ गया है। जयशंकर प्रसाद कृत ‘कामायनी में मनु को मन का, श्रद्धा को हृदय, इड़ा को बुद्धि का, देवगण को इन्द्रियों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में दीपक, फूल, आकाश, दर्पण, निर्झर आदि को प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है; यथा-निम्न पंक्तियों में दीपक को जीवन के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है-
मधुर मधुर मेरे दीपक जल ।
युग युग प्रतिदिन प्रतिरक्षण प्रतिपल,
प्रियतम का पथ आलोकित कर।
14. परिनिष्ठित, परिमार्जित खड़ीबोली का प्रयोग
छायावादी कवियों ने शुद्ध, परिनिष्ठित, परिमार्जित व साहित्यिक खड़ीबोली का अपनी काव्य-रचनाओं में प्रयोग किया है। फिर भी इनकी काव्य-भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। परन्तु यह अवश्य कहा जाएगा कि इन कवियों ने अपनी प्रतिभा से शब्दों को नए ढंग से प्रयुक्त करके छायावादी काव्य की भाषा को कलात्मक व काव्यात्मक बनाया।