Contents
Jai Shankar Prasad Ka Jivan Parichay: दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम हिंदी साहित्य के छायावाद को समृद्ध करने वाले जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने जा रहें है। उनके जीवन परिचय के साथ-साथ हम उनकी प्रमुख रचनाएँ और काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी जानेगें। तो आइये पढ़ते है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय।
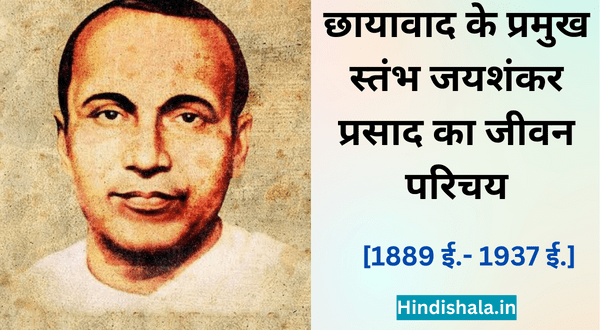
जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय
छायावाद के प्रवर्त्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य कुल में 30 जनवरी 1889 ई. में हुआ था। उनका कुल ‘सुँघनी साहू’ के नाम से विख्यात था। उनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। किशोरावस्था में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। प्रसाद जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया।
वे भारतीय साहित्य और संस्कृति के पुजारी थे तथा राष्ट्र-प्रेम की भावना उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। शैव दर्शन से प्रभावित होने के कारण वे नियतिवादी भी थे। यक्ष्मा रोग का शिकार होकर 15 नवंबर 1937 ई. में वे 48 वर्ष की आयु में ही इस संसार से विदा हो गए।
| नाम | जयशंकर प्रसाद |
| जन्म | 30 जनवरी 1889 ई. |
| जन्म स्थान | उत्तर प्रदेश के काशी में |
| पिता का नाम | श्री देवी प्रसाद |
| माता का नाम | श्रीमती मुन्नी देवी |
| पत्नी का नाम | श्रीमती कमला देवी |
| साहित्य में पहचान | छायावाद के एक स्तंभ |
| प्रमुख रचनाएँ | आँसू, कामायनी, कंकाल, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त |
| देहांत | 15 नवंबर 1937 ई. |
| जीवंत आयु | 48 वर्ष |
जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएँ
काव्य-ग्रंथ– ‘लहर’, ‘झरना’, ‘आँसू’, ‘कानन-कुसुम’, ‘प्रेम पथिक’, ‘महाराणा का महत्त्व’, ‘करुणालय, ‘चित्राघर’, ‘कामायनी’।
उपन्यास– ‘कंकाल’, ‘तितली’, ‘इरावती’, (अपूर्ण)।
कहानी-संग्रह– ‘छाया’, ‘प्रतिध्वनि’, ‘आकाशदीप’, ‘आँधी और इंद्रजाल’, (कुल 69 कहानियाँ)।
निबंध-संग्रह– ‘काव्य और कला तथा अन्य निबंध।
नाटक– ‘सज्जन’, ‘राज्यश्री’, ‘अजातशत्रु’, ‘एक घूँट’, ‘कल्याणी’, ‘परिचय’, ‘विशाख’, ‘कामना’, ‘स्कंदगुप्त’, ‘ध्रुवस्वामिनी’, और ‘चंद्रगुप्त।
इन्हें भी पढ़ें :-
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय
सुमित्रानंदन पंत जीवन परिचय PDF
महादेवी वर्मा जीवन परिचय पीडीऍफ़
जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएँ
प्रसाद जी एक प्रतिभासंपन्न साहित्यकार थे। वे छायावाद के प्रवर्त्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अतीत के प्रति उनका मोह था, लेकिन वर्तमान के प्रति भी वे जागरूक थे। उनके काव्य की विशेषताएँ इस प्रकार से हैं –
प्रेम तथा सौंदर्य का वर्णन
प्रसाद जी के काव्य का मुख्य तत्त्व प्रेमानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति है। प्रेमानुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक फैली हुई है। इसी प्रकार से प्रसाद जी ने मानव, प्रकृति और ईश्वर तीनों के सौंदर्य का आकर्षक चित्रण किया है। उनकी सौंदर्य-चेतना परिष्कृत,उदात्त एवं सूक्ष्म है।
वेदना की अभिव्यक्ति
प्रसाद जी के काव्य में ऐसे अनेक स्थल हैं जो पाठक के ह्रदय कप छू लेते हैं। उनका ‘आँसू’ काव्य कवि के ह्रदय की वेदना को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से ‘लहर’ काव्य-ग्रंथ की ‘प्रलय की छाया’ कविता भी मार्मिक है। ‘कामायनी’ में भी इस प्रकार के स्थलों की कमी नहीं है जो पाठक के ह्रदय को आत्मविभोर न कर देते हों।
प्रकृति-वर्णन
प्रसाद जी के काव्य में अनेक स्थलों पर प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। ‘लहर’ की अनेक कविताएँ प्रकृति-वर्णन से संबंधित हैं। प्राकृतिक पदार्थो पर मानवीय भावों का आरोप करना उनके प्रकृति-चित्रण की अनूठी विशेषता है ; जैसे—
बीती विभावरी जाग री,
अंबर पनघट में डुबो रही,
तारा घट उषा-नागरी।
छायावादी काव्य होने के नाते यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण देखने योग्य है। उषा को नायिका के रूप में वर्णित किए जाने से यहाँ प्रकृति मानवीकरण हुआ है। उन्होंने प्रकृति-वर्णन के अनेक रूपों में से आलंबन, उद्दीपन, दूती, उपदेशिका, रहस्यात्मक, प्रष्ठभूमि, मानवीकरण आदि रूपों को चुना है।
रहस्य भावना
छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद सर्वात्मवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं। वे अज्ञात सत्ता के प्रेम-निरूपण में अधिक तल्लीन रहे हैं। उनकी इस प्रवृति को रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। कवि बार-बार प्रश्न करता है कि वह अज्ञात सत्ता कौन है और क्या है ? प्रसाद जी के काव्य में रहस्य-भावना का सुष्ठु रूप देखने को मिलता है।
रहस्यसाधक कवि प्रकृति के अनंत सौंदर्य को देखकर उस विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा प्रकट करता है। तदंतर अपनी प्रिया का अधिकाधिक परिचय प्राप्त करने के लिए आतुरता व्यक्त करता है, उसके विरह में तड़पता है और प्रियतमा के परिचय की अनुभूति का ‘गूँगे के गुड़’ की भाँति आस्वादन करता है। प्रसाद जी के काव्य में रहस्य भावना का रूप निम्नलिखित उदाहरण में देखा जा सकता है –
हे अनंत रमणीय! कौन हो तुम ?
यह मैं कैसे कह सकता।
कैसे हो, क्या हो? इसका तो
भार विचार न कह सकता।।
नारी भावना
छायावादी कवि होने के कारण प्रसाद जी ने नारी को अशरीरी सौंदर्य प्रदान करके उसे लोक की मानवी न बनाकर परलोक की ऐसी काल्पनिक देवी बना दिया जिसमें प्रेम, सौंदर्य, यौवन और उच्च भावनाएँ हैं, लेकिन ऐसे गुण मृत्युलोक की नारी में देखने को नहीं मिलते। ‘कामायनी’ की श्रद्धा इसी प्रकार की नारी है।
वह काल्पनिक जगत की अशरीरी सौंदर्यसंपन्न अलौकिक देवी है जो नित्य छवि से दीप्त है, विश्व की करुणा-कामना मूर्ति है और कानन-कुसुम अंचल में मंद पवन से प्रेरित सौरभ की साकार प्रीतमा है। प्रसाद जी की यह नारी भावना छायावादी काव्य के सर्वथा अनुकूल है लेकिन यह नारी भावना आधुनिक युगबोध से मेल नहीं खाती।
नवीन जीवन-दर्शन
कविवर प्रसाद शैव दर्शन के अनुयायी थे। अतः उनके दार्शनिक विचारों पर शैव दर्शन का स्पष्ट प्रभाव है। वे कामायनी के माध्यम से समरसता और आनंदवाद की स्थपना करना चाहते हैं। उनकी रचनाओं, विशेषकर,’कामायनी’ में दार्शनिकता और कवित्व का सूंदर समन्वय हुआ है। वे समरसताजन्य आनंदवाद को ही जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। ‘कामायनी’ यात्रा ‘चिंता’ सर्ग से प्रांरभ होकर ‘आनंद’ सर्ग में ही समाप्त होती है।
राष्ट्रिय भावना
प्रसाद सांस्कृति और दार्शनिक चेतना के कवि हैं। यह सांस्कृति चेतना उनके राष्ट्रिय भावों की प्रेरक। उनके नाटकों में कवि का देशानुराग अथवा राष्ट्र-प्रेम अधिक मुखरित हुआ है। उनकी काव्य-रचनाओं में यह राष्ट्र-प्रेम संस्कृति प्रेम के रूप में संकेतित हुआ है।
कवि ने अतीत के संदर्भ में वर्तमान का भी चित्रण किया है। ‘चन्द्रगुप्त’ ‘स्कंदगुप्त’ ‘ध्रुवस्वामनी’, ‘जनमेजय का नागयज्ञ’ आदि नाटकों में भी इसी दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया है। ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक निम्नलिखित गीत कवि की राष्ट्रिय भावना को स्पष्ट करता है –
अरुण यह मधुमय देश हमारा।
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।
सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर,
छिटका जीवन-हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा।
मानवतावादी दृष्टिकोण
मानवतावादी छायावादी कवियों की उल्लेखनीय प्रवृति है। अनेक स्थलों पर कवि राष्ट्रीयता की भाव-भूमि से ऊपर उठकर मानव-कल्याण की चर्चा करता हुआ दिखाई देता है। प्रसाद जी के काव्य में शाश्वत मानवीय भावों और मानवतावाद को प्रचुर बल मिला है। ‘कामायनी’ में कवि ने मनु, श्रद्धा और इड़ा के प्रतीकों के माध्यम से मानवता के विकास की कहानी कहि है और इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान के समन्वय पर बल दिया है। समष्टि के लिए व्यक्ति का उत्सर्ग ‘कामायनी’ का संदेश है। श्रद्धा इस बात पर देती हुई कहती है –
औरों को हँसते देखो मनु हँसो और सुख पाओ।
अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ।।
‘आनंद’ सर्ग में कवि ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की चर्चा करके विश्व-वंधुत्व की भावना का संदेश दिया है। कवि बार-बार मानव-प्रेम पर बल देता है और मानवतावादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है।
जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली
प्रसाद जी ने प्रबंध और निति इन दो काव्य-रूपों को ही अपनाया। ‘प्रेम पथिक’ और ‘महाराणा का महत्त्व’ दोनों उनकी प्रबंधात्मक रचनाएँ है। ‘कामायनी’ उनका प्रिसिद्ध महाकाव्य है। ‘लहर’, ‘झरना’ और ‘आँसू’ गीतिकाव्य है। उनके काव्य में भावात्मकता, संगीतात्मकता, आत्माभिव्यक्ति, संक्षिप्तता, कोमलकांत पदावली आदि सभी विशेषताएँ देखी जा सकती हैं। प्रसाद जी की भाषा साहित्यिक हिंदी है। फिर भी इसे संस्कृतनिष्ठ, तत्सम प्रधान हिंदी भाषा कहना अधिक उचित होगा।
प्रसाद जी की भाषा में ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुण विधमान हैं। उनकी भाषा प्रवाहपूर्ण, प्रांजल, संगीतात्मक और भावनाकूल है। उनकी भाषा की प्रथम विशेषता है–लाक्षणिकता। लाक्षणिक प्रयोगों में कवि ने विरोधाभास, मानवीकरण, विशेषण-विपर्यय, प्रतीक आदि उपकरणों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। उनकी भाषा की दूसरी विशेषता है— प्रतिकात्मकता। कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों को प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। उनके सभी प्रतीक प्रभावपूर्ण है। कवि ने कुछ स्थलों पर चित्रात्मकता और ध्वन्यात्मकता का भी सफल प्रयोग है।
प्रसाद जी की अलंकार योजना उच्चकोटि की है। शब्दालंकारों की उत्प्रेक्षा अर्थालंकारों में उनकी दृष्टि अधिक रमी है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति,अर्थान्तरन्यास आदि प्रसाद जी के प्रिय अलंकर हैं। प्रसाद जी की छंद योजना स्वर और लय की मिठास से अणुप्राणित है। कुछ स्थलों पर कवि ने अतुकांत और मुक्तक छंदो का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उनका काव्य उच्चकोटि का है।