Contents
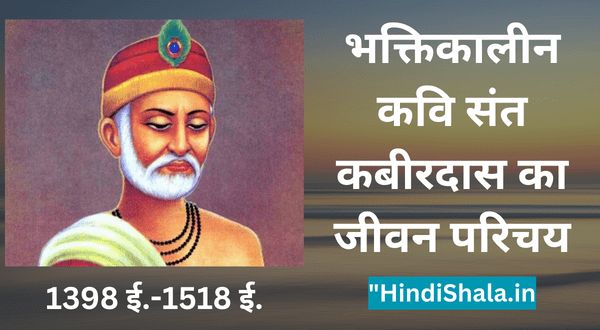
संत कबीर जीवन परिचय
कबीर में सन्त तथा समाज सुधारक दोनों के गुण विद्यमान थे। ये सिकन्दर लोदी के समकालीन थे। कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान होता है। कबीरदास भारत के भक्ति काव्य परंपरा के महानतम कवियों में से एक थे। भारत में धर्म, भाषा या संस्कृति कबीर के बगैर पूरी नहीं मानी जाती है। कबीरपंथी, एक धार्मिक समुदाय हैं जो कबीर के सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपनी जीवन शैली का आधार मानते हैं। सन्त कबीर का जन्म लहरतारा के पास सन् 1398 ई. में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ तथा जुलाहा परिवार में इनका पालन पोषण हुआ।
कबीर संत रामानंद के शिष्य बने और अलख जगाने लगे। कबीर सधुक्कड़ी भाषा में किसी भी सम्प्रदाय और रूढ़ियों की परवाह किये बिना खरी बात कहते थे। कबीर की वाणी उनके मुखर उपदेश उनकी साखी, रमैनी, बीजक, बावन-अक्षरी, उलटवासी में देखे जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में उनके 200 पद और 250 साखियाँ हैं। काशी में प्रचलित मान्यता है कि जो यहाँ मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कबीर रूढ़िवादिता के सख्त खिलाफ थे। काशी छोड़ मगहर चले गये और सन् 1518 ई. के आस पास वहीं देह त्याग किया। मगहर में कबीर की समाधि है जिसे हिन्दू मुसलमान दोनों पूजते हैं।
कबीरदास संक्षिप्त जीवनी
| नाम | कबीरदास |
| जन्म | 1398 ई. |
| जन्म स्थान | लहरतारा (उत्तर प्रदेश ) |
| पिता का नाम | नीरू |
| माता का नाम | नीमा |
| पत्नी का नाम | लोई |
| निधन | 1518 ई. |
इन्हें भी पढ़ें :-
कबीर की भक्ति भावना
तुलसीदास का जीवन परिचय
कबीर के जन्म संबंधी किंवदन्तियाँ
हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीर का व्यक्तित्व अनुपम है। गोस्वामी तुलसीदास के अलावा इतना महिमामण्डित व्यक्तित्व कबीर के सिवा अन्य किसी का नहीं है। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदन्तियाँ हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे जगद्गुरु रामानन्द स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे।
ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आयी। उसे नीरु नाम का जुलाहा। अपने घर ले आया। उसी ने उसका पालन-पोषण किया। बाद में यही चालक कबीर कहलाया कुछ लोग उन्हें जन्म से मुसलमान मानते थे तथा युवावस्था में स्वामी रामानन्द के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई।
कबीर के ही शब्दों में हम काशी में प्रकट भये हैं, रामानंद चेताये
अन्य जनश्रुतियों से यह जानकारी मिलती है कि कबीर ने हिंदू-मुसलमान के मध्य भेद-भाव मिटा कर हिंदू-भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को अपना लिया।
जनश्रुति के अनुसार उन्हें एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाती थी। इतने लोगों की परवरिश करने के लिये उन्हें अपने करघे पर काफी काम करना पड़ता था। लगभग 120 वर्ष की आयु में उन्होंने मगहर में अपने प्राण त्याग दिये। उनका घर साधु संतों से भरा रहता था। कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे – मसि कागद छूवो नहीं, कलम गही नहिं हाथ।
कबीर की मगहर में मृत्यु संबंधी यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए।
उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुँह से माखे और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। आपके समस्त विचारों में रामनाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। उनके अनुसार ईश्वर एक है तथा ये कर्मकाण्ड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मसजिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे।
एच.एच. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर आठ ग्रंथ हैं। विशप, जी.एच. बेस्टकॉट ने कबीर के 84 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की तो रामदास गौड़ ने हिंदुत्व में 71 पुस्तकों के बारे में जानकारी प्रदान की है।
कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके तीन भाग हैं – रमैनी, सवद और साखी।
वह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूरबी, ब्रजभाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं।
कबीर के दोहे –
हरिमोर पिउ, मैं राम की बहुरिया तो कभी कहते हैं, हरि जननी में बालक तोरा ।
उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गयी। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुँच सके। इससे दोनों सम्प्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई। इनके पंथ • मुसलमान-संस्कृति और गोभक्षण के विरोधी थे। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है।
कबीर द्वारा बनारस का घर त्याग
वृद्धावस्था में यश और कीर्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्मपरीक्षण करने के लिये देश के विभिन्न भागों की यात्राएँ कीं। इसी क्रम में वे कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में पहुँचे। वहाँ रामकृष्ण का छोटा-सा मन्दिर था। वहाँ के संत भगवान् गोस्वामी के जिज्ञासु साधक थे किंतु उनके तर्कों का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। संत कबीर से उनका विचार-विनिमय हुआ।
कबीर की एक साखी ने उनके मन पर गहरा असर किया।
वन ते भागा विहरे पड़ा, करहा अपनी वान।
करहा वेदन कासों कहे, को करहा को जान।
अर्थात – वन से भाग कर बहेलिये के द्वारा खोये हुए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किससे कहे ?
सारांश यह कि धर्म की जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान गोसाई अपना घर छोड़कर बाहर तो निकल आये और हरिव्यासी सम्प्रदाय के गहे में गिर कर अकेले निर्वासित होकर असंवाद्य स्थिति में पड़ चुके हैं।
मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए उन्होंने एक साखी हाजिर कर दी
पाहन पूजे हरि मिलें, तो मैं पूजौं पहार।
वा ते तो चाकी भली, पीसी खाय संसार ।।
कबीर के राम
कबीर के राम तो अगम हैं और संसार के कण-कण में विराजते हैं। कबीर के राम इस्लाम के एकेश्वरवादी, एकसत्तावादी खुदा भी नहीं हैं। इस्लाम में ख़ुदा या अल्लाह को समस्त जगत एवं जीवों से भिन्न एवं परम समर्थ माना जाता है। पर कबीर के राम परम समर्थ भले हों, लेकिन समस्त जीवों और जगत से भिन्न तो कदापि नहीं हैं बल्कि इसके विपरीत वे तो सबमें व्याप्त रहने वाले रमता राम हैं।
व्यापक ब्रह्म सबनिमैं एकै को पंडित को जोगी।
रावण-राव कवनसूं। कवन वेद को रोगी।
कबीर राम की किसी खास रूपाकृति की कल्पना नहीं करते, क्योंकि रूपाकृति की कल्पना करते ही राम किसी खास ढाँचे (फ्रेम) में, बँध जाते, जो कबीर को किसी भी हालत में मंजूर नहीं कबीर राम की अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक स्वरूप देना चाहते थे। इसके कुछ विशेष कारण थे, जिनकी चर्चा हम इस लेख में आगे करेंगे। किन्तु इसके बावजूद कबीर राम के साथ एक व्यक्तिगत पारिवारिक किस्म का संबंध जरूर स्थापित करते हैं। राम के साथ उनका प्रेम उनकी अलौकिक और महिमाशाली सत्ता को एक क्षण भी भुलाए बगैर सहज प्रेमपरक मानवीय संबंधों के धरातल पर प्रतिष्ठित है।
रूप की बजाय नाम पर बल
कबीर नाम में विश्वास रखते हैं, रूप में नहीं। हालांकि भक्ति-संवेदना के सिद्धांतों में यह बात सामान्य रूप से प्रतिष्ठित है कि ‘नाम रूप से ‘बढ़कर है’, लेकिन कबीर ने इस सामान्य सिद्धांत का क्रांतिधर्मी उपयोग किया। कबीर ने राम-नाम के साथ लोकमानस में शताब्दियों से रचे-बसे संश्लिष्ट भावों को उदात्त एवं व्यापक स्वरूप देकर उसे पुराण-प्रतिपादित ब्राह्मणवादी विचारधारा के खाँचे में बाँधे जाने से रोकने की कोशिश की। कबीर के राम निर्गुण-सगुण के भेद से परे हैं।
दरअसल उन्होंने अपने राम को शास्त्र-प्रतिपादित अवतारी, सगुण, वर्चस्वशील वर्णाश्रम • व्यवस्था के संरक्षक राम से अलग करने के लिए ही ‘निर्गुण राम’ शब्द का प्रयोग किया- ‘निर्गुण राम जपहु रे भाई।’
इस ‘निर्गुण’ शब्द को लेकर भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। कबीर का आशय इस शब्द से सिर्फ इतना है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, गुण, काल आदि की सीमाओं में बाँधा नहीं जा सकता। जो सारी सीमाओं से परे हैं और फिर भी सर्वत्र हैं, वही कबीर के निर्गुण राम हैं।
इसे उन्होंने ‘रमता राम’ नाम दिया है। अपने राम को निर्गुण विशेषण देने के बावजूद कबीर उनके साथ मानवीय प्रेम संबंधों की तरह के रिश्ते की बात करते हैं। कभी वह राम को माधुर्य भाव से अपना प्रेमी या पति मान लेते हैं तो कभी दास्य भाव से स्वामी। कभी-कभी वह राम को वात्सल्य मूर्ति के रूप में माँ मान लेते हैं और खुद को उनका पुत्र ।
निर्गुण-निराकार ब्रह्म के साथ भी इस तरह का सरस, सहज, मानवीय प्रेम कबीर की भक्ति की विलक्षणता है। यह दुविधा और समस्या दूसरों को भले हो सकती है कि जिस राम के साथ कबीर इतने, अनन्य, मानवीय संबंधपरक प्रेम करते हों, वह भला निर्गुण कैसे हो सकते हैं, पर खुद कबीर के लिए यह समस्या नहीं है। वह कहते भी हैं –
“संती, धोखा कासूं कहिये। गुनमैं निरगुन, निरगुनमैं गुन, बाट छांड़ि क्यूं बहिसे!” नहीं है।
प्रोफेसर महावीर सरन जैन ने कबीर के राम एवं कबीर की साधना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है: ‘कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ।
कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से आरम्भ होती है। वे किसी के शिष्य नहीं, रामानन्द द्वारा चेताये हुए चेला हैं। उनके लिए राम रूप नहीं हैं, दशरथी राम नहीं हैं, उनके राम तो नाम साधना के प्रतीक है। उनके राम किसी सम्प्रदाय, जाति या देश की सीमाओं में कैद नहीं हैं। प्रकृति के कण-कण में, अंग-अंग में रमण करने पर भी जिसे अनंग स्पर्श नहीं कर सकता, वे अलख, अविनाशी, परम तत्व ही राम हैं। उनके राम मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भेद-भाव के कारक नहीं हैं। वे तो प्रेम तत्व के प्रतीक हैं।
भाव न होकर महाभाव की आराधना
‘प्रेम जगावै विरह को, विरह जगावै पीउ, पीउ जगावै जीव को, जोइ पीउ सोई जीउ जो पीउ है, वही जीव है।
इसी कारण उनकी पूरी साधना “हंस उबारन आए की साधना है। इस हंस का उबारना पोथियों के पढ़ने से नहीं हो सकता, ढाई आखर प्रेम के आचरण से ही हो सकता हैं। धर्म ओढ़ने की चीज नहीं है, जीवन में आचरण करने की सतत सत्य साधना है।
उनकी साधना प्रेम से आरम्भ होती है। इतना गहरा प्रेम करो कि वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। उसको पाने की इतनी उत्कंठा हो जाए कि सबसे वैराग्य हो जाए, विरह भाव हो जाए तभी उस ध्यान समाधि में पीउ जाग्रत हो सकता है। वही पीउ तुम्हारे अन्तर्मन में बैठे एक जीव को जगा सकता है। जोई पीउ है सोई जीउ है।
तब तुम पूरे संसार से प्रेम करोगे, तब संसार का प्रत्येक जीव तुम्हारे प्रेम का पात्र बन जाएगा। सारा अहंकार, सारा द्वेष दूर हो जाएगा। फिर महाभाव जगेगा। इसी महाभाव से पूरा संसार पिउ का घर हो जाता है।
सूरज चन्द्र का एक ही उजियारा, सब यहि पसरा ब्रह्म पसारा ।