Contents
- महादेवी वर्मा का जीवन परिचय
- Mahadevi Verma Jivan Parichay
- महादेवी वर्मा की संक्षिप्त जीवनी
- शिक्षा-दीक्षा
- वैवाहिक जीवन
- महिला कवि सम्मेलन की शुरुआत
- महिला शिक्षा प्रमुख उद्देश्य
- महादेवी वर्मा रचनाएँ
- महादेवी वर्मा साहित्यिक विशेषताएँ
- समाज का यथार्थ चित्रण
- निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति
- मानवेतर प्राणियों के प्रति प्रेम-भावना
- करुणा एवं प्रेम-भावना का चित्रण
- समाज सुधार की भावन
- वात्सल्य भावना का चित्रण
- महादेवी वर्मा की भाषा शैली
- निधन वर्ष
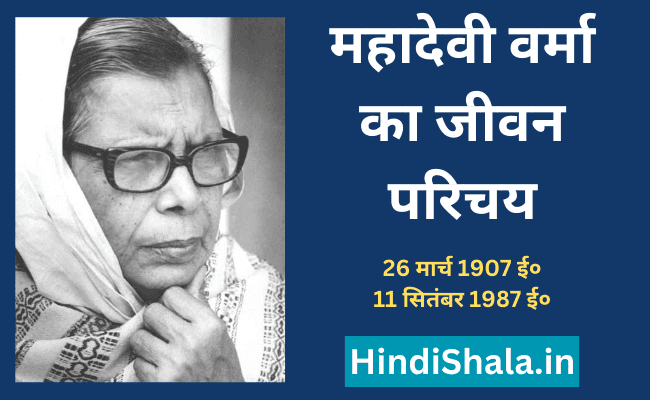
महादेवी वर्मा का जीवन परिचय
महादेवी वर्मा (1907-1987) को हिन्दी साहित्य की सबसे प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक माना जाता है। वे हिन्दी साहित्य में छायावादी युग’ के चार प्रमुख स्तंभों, में एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिन्दी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिन्दी के विशाल मन्दिर की सरस्वती भी कहा है।
महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता से पूर्व भारत तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भी भारत देखा था। वे उन कवयित्रियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अन्धकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा समाज-सुधार तथा महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास भी किया।
उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। महादेवी वर्मा ने ब्रजभाषा के समान ही खड़ी बोली हिन्दी की कविता में भी कोमलता लाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिन्दी का जामा पहनाया। महादेवी जी छायावाद के चार स्तंभो में से एक हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है :-
महादेवी वर्मा ही छायावादी कहे जाने वाले कवियों में रहस्यवाद के भीतर रही हैं।
Mahadevi Verma Jivan Parichay
संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद-सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने अपना ज्यादातर समय अध्यापन में व्यतीत किया तथा अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में कार्य करती रहीं। उनका बाल-विवाह हुआ परंतु उन्होंने अविवाहिता की भांति जीवन-यापन किया।
प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ-साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थीं। वे हिन्दी साहित्य के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रहीं। वर्ष 2007 उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया।
महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च, 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या सात पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबा बाबू बाँके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का, नाम महादेवी रखा। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में पढ़ाने का कार्य किया करते थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था।
हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थीं। विवाह के समय अपने साथ सिंहासनासीन भगवान की मूर्ति भी लायी थीं। वे प्रतिदिन कई घंटे पूजा-पाठ तथा रामायण, गीता तथा विनय पत्रिका का पाठ किया करती थीं एवं संगीत से उन्हें काफी लगाव था। इसके बिल्कुल विपरीत उनके पिता गोविन्द प्रसाद वर्मा सुन्दर, विद्वान, संगीत प्रेमी, नास्तिक, शिकार करने एवं घूमने के शौकीन, मांसाहारी तथा हँसमुख व्यक्ति थे। सुमित्रानंदन पन्त तथा निराला को भाई समान स्नेह करती थीं तथा उन्हें राखी भी बाँधती थी। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता थी, उनकी पुष्ट कलाइयों में महादेवी जी लगभग चालीस वर्षों तक राखी बाँधती रहीं।
महादेवी वर्मा की संक्षिप्त जीवनी
| नाम | महादेवी वर्मा |
| उपनाम | आधुनिक मीरा, वेदना की कवयित्री, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी |
| जन्म | 26 मार्च, 1907 ई. |
| जन्म स्थान | फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश |
| पिता का नाम | गोविन्द प्रसाद वर्मा |
| माता का नाम | हेमरानी देवी |
| पति का नाम | डॉ. सवरूप नारायण वर्मा |
| पेशा | उपन्यासकार, कवयित्री, लघुकथा लेखिका |
| प्रमुख सम्मान व पुरस्कार | ज्ञानपीठ पुरस्कार (1982) भारत भारती (1943) पदम भूषण (1956) पद्म विभूषण (1988) मरणोपरांत |
| साहित्यिक काल | छायावाद |
| प्रमुख रचनाएँ | पथ के साथी, मेरा परिवार |
| निधन | 11 सितंबर, 1987 ई. |
शिक्षा-दीक्षा
महादेवी वर्मा की स्कूली शिक्षा इंदौर मिशन में स्कूल में आरंभ हुई थी। उन्हें, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाहोपरान्त महादेवी जी ने 1919 में क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रवास में रहने लगीं। महादेवी वर्मा 1921 के दौरान आठवीं कक्षा में पूरे प्रान्त में प्रथम आई थी। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की।
वे सात वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थीं और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज के दिनों में सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी अच्छी सहेली बन चुकी थीं। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम.ए. पास किया तब तक उनके दो कविता संग्रह ‘नीहार’ तथा ‘रश्मि’ प्रकाशित हो चुके थे।
वैवाहिक जीवन
इनका विवाह सन् 1916 में श्री स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, जो उस समय दसवीं कक्षा के विद्यार्थी थे। श्री वर्मा इण्टर करके लखनऊ, मेडिकल कॉलेज में बोडिंग हाउस में रहने लगे। महादेवी जी उस समय क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद के छात्रवास में थीं। महादेवी वर्मा को वैवाहिक जीवन व्यतीत करना पसंद नहीं था। कारण कुछ भी रहा हो पर श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कोई वैमनस्य नहीं था। सामान्य स्त्री-पुरुष के में उनके संबंध मधुर ही रहे।
दोनों में कभी-कभी पत्राचार भी होता था। यदा-कदा श्री वर्मा इलाहाबाद में उनसे मिलने भी आते थे। श्री वर्मा ने महादेवी जी के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी जी सन्यासिनी रूपी जीवन व्यतीत करती थीं तथा आजीवन श्वेत वस्त्र धारण करती रहीं, तख्त पर सोईं और कभी शीशा नहीं देखा। 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे स्थाई रूप से इलाहाबाद में रहने लगीं।
महिला कवि सम्मेलन की शुरुआत
भारत में महिला कवि सम्मेलन की शुरुआत सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा की गई थी। इस प्रकार का पहला अखिल भारतवर्षीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला, विद्यापीठ में संपन्न हुआ। वे हिंदी साहित्य में रहस्याद की प्रवर्तिका भी मानी जाती हैं। महादेवी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थीं । महात्मा गाँधी से प्रेरणा लेकर वे जनसेवा के कार्यों में लग गईं, जिसके अंतर्गत उन्होंने झूसी तथा आजादी के दौरान महत्त्वपूर्ण योगदान किया। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कसबे के उमागढ़ नामक गाँव में महादेवी वर्मा ने एक बँगला बनवाया था। जिसका नाम उन्होंने मीरा मंदिर रखा था। जितने दिन वे यहाँ रहीं इस छोटे से गाँव की शिक्षा और विकास के लिए काम करती रहीं।
महिला शिक्षा प्रमुख उद्देश्य
महिलाओं को शिक्षित तथा आत्मनिर्भर बनाना मुख्य उद्देश्य था । आजकल इस बंगले को महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। श्रृंखला की कड़ियाँ में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस व दृढ़ता से आवाज उठाई हैं और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया।
शिक्षा के क्षेत्र में तथा स्त्रियों के सर्वांगीण विकास हेतु जो कार्य किये जिन्हें देखते हुए उन्हें समाज सुधारक कहना गलत नहीं होगा। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के कहीं दर्शन नहीं होते बल्कि अदम्य रचनात्मक रोष समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है। अपने जीवन का ज्यादातर समय उन्होंने इलाहाबाद नगर में व्यतीत किया।
महादेवी वर्मा रचनाएँ
महादेवी वर्मा अध्यापन, संपादन तथा लेखन के क्षेत्र में ही कार्य ) करती रहीं। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। यह कार्य अपने समय में महिला-शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका ‘चाँद’ में 1932 के दौरान एक संपादक के रूप में कार्यभार सँभाला। 1930 में नीहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा, तथा 1936 में सांध्यगीत नामक उनके चार कविता संग्रह प्रकाशित हुए।
1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ वृहदाकार में ‘यामा’ शीर्षक से प्रकाशित किया गया। उन्होंने शिक्षा, चित्रकला, गद्य तथा काव्य आदि सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियाँ हैं जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में सन् 1955 के दौरान साहित्यकार संसद की शुरुआत की तथा पं. इलाचंद्र जोशी के सहयोग से ‘साहित्यकार’ का संपादन सँभाला। यह इस संस्था का मुखपत्र था ।
उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं:-
- नीहार (1930)
- रश्मि (1932)
- नीरजा (1934)
- सांध्यगीत (1986)
- दीपशिखा (1912)
- सप्तपर्णा (अनूदित-1959)
- प्रथम आयाम (1974)
- अग्निरेखा (1990)
श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित कई काव्य संकलनों का प्रकाशन हो चुका है, जिनमें उपर्युक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किये गये हैं, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, सन्धिनी (1965), यामा (1936), गीतपर्व, दीपगीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी आदि।
- रेखाचित्रः अतीत के चलचित्र (1941) और स्मृति की रेखाएँ(1943),
- संस्मरणः पथ के साथी (1956) और मेरा परिवार (1972 और संस्मरण (1983)
- ललित निबंध: क्षणदा (1956)
- चुने हुए भाषणों का संकलनः संभाषण (1974)
- निबंधः श्रृंखला की कड़ियाँ (1942), विवेचनात्मक गद्य (1942), साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध (1962), संकल्पिता (1969)
- कहानियाँ: गिल्लू
- संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रहः हिमालय (1963),
- काव्य संग्रह: दीपशिखा, यामा, नीहार, नीरजा, रश्मि, सांध्यगीत।
- आलोचना: विभिन्न काव्य संग्रहों की भूमिकाएँ, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य ।
- संपादन – चाँद, आधुनिक कवि काव्यमाला आदि।
महादेवी वर्मा साहित्यिक विशेषताएँ
महादेवी वर्मा जी आधुनिक हिंदी-साहित्य की मीरा मानी जाती हैं। वे छायावाद की महान् कवयित्री हैं लेकिन काव्य के साथ-साथ गद्य में भी उनका महान् योगदान रहा है। वे एक साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। उनका पद्य साहित्य जितना अधिक आत्मकेंद्रित है, गद्य साहित्य उतना ही समाज केंद्रित है। महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
समाज का यथार्थ चित्रण
महादेवी वर्मा जी ने अपने गद्य साहित्य में समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। काव्य में जहाँ उन्होंने अपने सुख-दुःख, वेदना आदि का चित्रण किया है वहीं गद्य में समाज के सुख-दुःख, ग़रीबी, शोषण आदि का यथार्थ वर्णन किया है। इनके रेखाचित्रों एवं संस्मरणों में समाज में फैली गरीबी, कुरीतियों, जाति-पाति, भेदभाव, धर्म संप्रदायवाद आदि विसंगतियों का यथार्थ के धरातल पर अंकन हुआ है। वे एक समाज सेवी लेखिका थीं। अतः आजीवन साहित्य सेवा के साथ-साथ समाज का उद्धार करने भी लगी रहीं।
निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति
महादेवी जी एक कोमल हृदय लेखिका थीं। उनके जीवन पर महात्मा बुद्ध विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि के विचारों का गहन प्रभाव पड़ा जिसके कारण उनकी निम्न वर्ग के प्रति गहन सहानुभूति रही है। उनके गद्य साहित्य में समाज के पिछड़े वर्ग के अत्यंत मार्मिक चित्र चित्रित हैं। उन्होंने समाज के उच्च वर्ग द्वारा उपेक्षित कहे जाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यही कारण है कि उन्होंने अपने गद्य । साहित्य में अधिकांश पात्र निम्न वर्ग से ग्रहण किए हैं।
मानवेतर प्राणियों के प्रति प्रेम-भावना
महादेवी जी केवल मानव प्रेमी नहीं थीं बल्कि अन्य प्राणियों से भी उनका गहन लगाव था। उन्होंने अपने घर में भी कुत्ते, बिल्ली, गाय, नेबला आदि को पाला हुआ था। इनके रेखाचित्रों एवं संस्मरणों में इन मानवेतर प्राणियों के प्रति इनका गहन प्रेम और संवेदना झंकृत होता है। जैसे- ‘लूसी के लिए सभी रोए परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था, वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। एक दिन पहले उसकी आँखें खुली थीं, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहा। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधवने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के समीप्य सुख के भ्रम में सो गया।
करुणा एवं प्रेम-भावना का चित्रण
महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य की मूल संवेदना करुणा एवं प्रेम है। इनके साहित्य पर बुद्ध की करुणा एवं दुःखवाद का गहन प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि इनके गद्य साहित्य में मानव एवं मानवेतर प्राणियों के प्रति करुणा एवं प्रेम भावना अत्यंत सजीव हो उठी है।
समाज सुधार की भावन
महादेवी जी एक समाज सेवी भावना से ओत-प्रोत महिला थी। उनके जीवन पर बुद्ध, विवेकानंद आदि विचारकों का बहुत प्रभाव पड़ा जिसके कारण उनकी वृत्ति समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई थी। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, विसंगतियों, विडंबनाओं आदि को उखाड़ने के भरपूर प्रयास किए हैं। इन्होंने अपने गद्य साहित्य में नारी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया है तथा नारी शोषण, बाल-विवाह आदि बुराइयों का खुलकर खंडन किया है।
वात्सल्य भावना का चित्रण
महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य में वात्सल्य रस का अनूठा चित्रण हुआ है। उनको मानव ही नहीं मानवेतर प्राणियों से भी वत्सल प्रेम था। वे अपने घर में पाले हुए कुत्ते, बिल्लियों, नेवला, गाय आदि प्राणियों की एक माँ के समान सेवा करती थीं। यही प्रेम और सेवा भावना उनके रेखाचित्र और संस्मरणों में भी अभिव्यक्त हुई है। लूसी नामक कुतिया की मृत्यु होने पर लेखिका एक माँ की तरह बिलख-बिलख रो पड़ी थी।
महादेवी वर्मा की भाषा शैली
महादेवी वर्मा जी एक श्रेष्ठ कवयित्री होने के साथ-साथ कुशल लेखिका भी थी। काव्य के साथ इसका गद्य साहित्य अत्यंत उत्कृष्ट है। इनके गद्य साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है। जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तद्भव तथा साधारण बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का समायोजन हुआ है।
इनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। महादेवी वर्मा ने अपने निबंधों, रेखाचित्रों और संस्मरणों में अनेक शैलियों को स्थान दिया है। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, समीक्षात्मक, संस्मरणात्मक, इतिवृत्तात्मक, व्यंग्यात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्म स्पर्शिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है।
वर्मा जी ने भाव प्रधान रेखाचित्र को भी इतिवृत्तात्मक शिल्प से मंडित किया है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के कारण इनकी भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। कहीं-कहीं अलंकारयुक्त शैली का प्रयोग भी हुआ है। वहाँ इनकी भाषा में अधिक प्रवाहमयता और सजीवता उत्पन्न हो गई है।
इनकी भाषा पाठक के विषय से तारतम्य स्थापित कर उसके हृदय पर अमिट छाप छोड़ देती है। में विशेष स्थान रखता है। संभवतः भाषा शैली की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ उत्कृष्ट हैं। वस्तुतः महादेवी वर्मा जी प्रतिष्ठित कवयित्री होने के साथ महान् लेखिका भी थीं। उनका गद्य साहित्य हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता हैं।
निधन वर्ष
11 सितंबर, 1987 को प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में रात 9 बजकर 30 मिनट पर उनका देहांत हो गया। महादेवी वर्मा में कवयित्री के साथ-साथ एक विशिष्ट गद्यकार के सभी गुण मौजूद थे।
इन्हें भी पढ़ें :-
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय
सुमित्रानंदन पंत जीवन परिचय
जय शंकर प्रसाद जीवन परिचय