Contents
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जीवन परिचय
- Ramchandra Shukla Ka Jivan Parichay
- रामचन्द्र शुक्ल की प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की साहित्यिक विशेषताएँ
- 1. मौलिक चिन्तन
- 2. सुगठित विचार परम्परा
- 3. गम्भीर विवेचन
- 4. हृदय और बुद्धि का समन्वय
- 5. अनुभूति पक्ष
- 4. प्रकृति वर्णन
- रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा-शैली
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जीवन परिचय
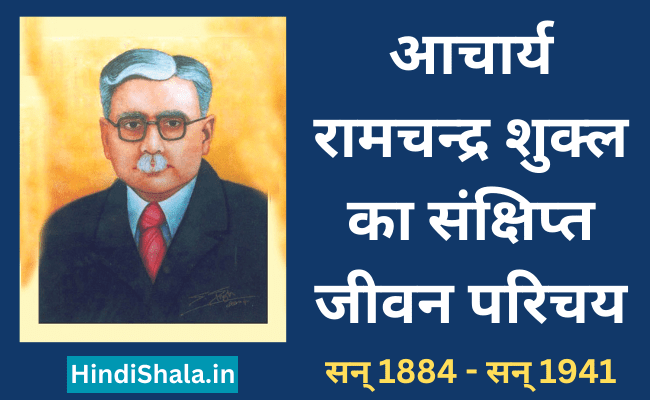
हिन्दी-साहित्य के प्रमुख निबंधकार एवं आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जन्म सन् 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चन्द्रबली था। प्रारम्भिक शिक्षा मिर्जापुर के जुबली स्कूल से प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने मिशन हाई स्कूल से फाइनल की परीक्षा पास की। परन्तु वे आगे पढ़ाई जारी न रख सके। कुछ समय के लिए उन्होंने मिशन हाई स्कूल में ही चित्रकला अध्यापक के रूप में शिक्षण कार्य किया तथा वे नायब तहसीलदार भी चुने गए।
परन्तु शीघ्र ही उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। सन् 1908 में वे नागरी प्रचारिणी सभा के ‘हिन्दी शब्द सागर’ शीर्षक शब्दकोश निर्माण में सह-सम्पादक के रूप में नियुक्त हुए। इसके अतिरिक्त वे काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक व सन् 1937 ई. में बाबू श्यामसुंदर के अपने अवकाश ग्रहण करने पर हिन्दी विभागाध्यक्ष भी रहे। सन् 1941 में हिन्दी की इस महान् विभूति का स्वर्गवास हो गया।
Ramchandra Shukla Ka Jivan Parichay
| नाम | रामचंद्र शुक्ल |
| जन्म | 4 अक्टूबर सन् 1884 ई. |
| जन्म स्थान | बस्ती जिले का अगोना ग्राम |
| पिता का नाम | चंद्रबली शुक्ल |
| शिक्षा-दीक्षा | हाई स्कूल फाइनल |
| व्यवसाय | चित्रकला अध्यापक, हिंदी अध्यापक, लेखक |
| साहित्य में स्थान | आलोचना सम्राट |
| लेखन विधा | आलोचना, निबंध, पत्रिका काव्य, इतिहास आदि। |
| प्रसिद्ध पुस्तक | हिंदी साहित्य का इतिहास |
| निधन | सन् 1941 ई. |
| जीवन आयु | लगभग 57 वर्ष |
रामचन्द्र शुक्ल की प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ
आचार्य शुक्ल ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी चलाई।
उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित है:-
(i) कहानियाँ – ग्यारह वर्ष का समय।
(ii) काव्य – रचना बुद्ध-चरित, अभिमन्यु वध
(iii) निबंध – उनके समस्त निबन्ध ‘चिंतामणि (दो भागों में संकलित हैं।
(iv) आलोचना – काव्य में रहस्यवाद, सूरदास, तुलसीदास व जायसी के साहित्य की समीक्षाएँ तथा हिन्दी साहित्य का इतिहास आदि।यह एक निर्विवाद सत्य है कि आचार्य शुक्ल को सर्वाधिक सफलता निबन्ध व आलोचना के क्षेत्र में ही मिली।
उन्होंने प्रायः भाव और मनोविकार, साहित्य तथा समीक्षा के भी सफल निबन्ध लिखे हैं। आचार्य शुक्ल जी के विचार-प्रधान निबन्ध तत्कालीन ‘सरस्वती’ तथा ‘आनन्द कादम्बिनी’ आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे।
उनके निबन्ध साहित्य के बारे में डॉ. श्याम सुन्दर दास ने उचित ही लिखा है-
“इनके निबन्ध अधिकांश गूढ़ एवं जटिल होते थे। उनसे चाहे साधारण हिन्दी पाठकों का मनोरंजन न होता हो, पर हिन्दी की उच्च शिक्षा के लिए वे आगे चलकर बड़े काम के होंगे।”
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की साहित्यिक विशेषताएँ
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार एवं आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने अधिक निबन्ध तो नहीं लिखे, लेकिन जितने भी लिखे हैं, ये उनकी ख्याति के लिए पर्याप्त हैं। मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा-भक्ति, करुणा, ला और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, घृणा, भय, क्रोध आदि प्रमुख हैं। कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति चित्रवाद आदि इनके कुछ उल्लेखनीय समीक्षात्मक निबन्ध हैं। शुक्ल जी के निबन्धों की विशेषताएं इस प्रकार हैं।
1. मौलिक चिन्तन
शुक्ल जी अपने मौलिक प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जिस किसी विषय पर निबन्ध लिखा है, उसके बारे में अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। उदाहरण के रूप में ‘श्रद्धा-भक्ति’ अथवा ‘कविता क्या है’ आदि निबन्धों को लिया जा सकता है। ‘श्रद्धा-भक्ति’ में उन्होंने पहले श्रद्धा की परिभाषा दी है। तत्पश्चात् उन्होंने श्रद्धा और प्रेम में अन्तर बताया है और फिर कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इसी प्रकार से शुक्ल जी ने ‘कविता क्या है, नामक निबन्ध में कविता के बारे में अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी की यह मौलिकता प्रत्येक निबन्ध में देखी जा सकती है।
2. सुगठित विचार परम्परा
शुक्ल जी के निबन्धों की अगली विशेषता यह है कि उनके निबन्धों में हमें सुगठित विचार-परम्परा देखने को मिलती है। पाठक निबन्ध को पढ़ते समय एक विचार से दूसरे विचार तक सहज रूप से पहुँच जाता है। कारण यह है कि उनके निबन्धों के विचार श्रृंखलावत् सुसम्बद्ध हैं। कहीं पर कोई बिखराव नहीं है। ‘कविता क्या है?” निबन्ध में वे कविता की परिभाषा देने के पश्चात् कविता और प्रकृति, कविता और अलंकार आदि विभिन्न विचारों के बारे में अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत करते हैं। पूरा निबन्ध पढ़ने के पश्चात् पाठक विषय का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
3. गम्भीर विवेचन
गम्भीर विवेचन उनके निबन्धों की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। शुक्ल जी ने जिस किसी विषय पर निबन्ध लिखा हो उस विषय के बारे में वे अपना गम्भीर विवेचन ही प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप उनके निबन्ध प्रभावशाली, मनोरंजक और आकर्षक बन जाते हैं। यह सब लेखक के गहन अध्ययन, गम्भीर चिन्तन और व्यावहारिक जीवन का परिणाम है। लेकिन वे अपने निबन्धों को नीरस नहीं बनने देते। यत्र-तत्र अपनी संवेदनशीलता का मिश्रण करते हुए चलते हैं।
4. हृदय और बुद्धि का समन्वय
शुक्ल जी के निबन्धों को लेकर अक्सर यह चर्चा की जाती है कि उनके निबन्ध हृदय प्रधान अथवा बुद्धि प्रधान हैं। स्वयं शुक्ल जी ने स्वीकार किया है कि उनके निबन्धों में हृदय एवं बुद्धि मणिकांचन का संयोग है। बुद्धि तत्त्व के कारण जब वे निबन्धों में विचारों का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं तो एक के बाद एक विचारों की श्रृंखला -सी बन जाती है। परन्तु अपने निबन्धों को रोचक बनाने के लिए यत्र-तत्र कल्पना का भी प्रयोग करने लगते हैं। फलस्वरूप उनके निबन्धों में सरसत्ता एवं मधुरता उत्पन्न हो जाती है एक चित्र द्रष्टव्य है-“एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूँकते-फूंकते थक गए। जब आग न जली तो उस पर कोप करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए।” इस प्रकार शुक्ल जी ने यत्र-तत्र हृदय एवं बुद्धि का सुन्दर समन्वय किया है।
5. अनुभूति पक्ष
यद्यपि शुक्ल जी के निबन्धों में बुद्धि तत्व की प्रधानता है, लेकिन उनमें अनुभूति तत्त्व की प्रखरता एवं प्रौढ़ता देखी जा सकती है। विशेषकर शुक्ल जी के मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध उनकी प्रौढ़ एवं प्रांजल अनुभूति के परिचायक हैं। उनमें वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुभूति बड़ी कुशलता के साथ व्यक्त हुई है। वे ‘उत्साह’ नामक निबन्ध में लिखते हैं-“जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसी की ओर उन्मुख कर्म होता है। कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है।” इसी प्रकार से मोटे आदमियों की चर्चा करते हुए वे अपना मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
4. प्रकृति वर्णन
शुक्ल जी को प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने अपने विभिन्न निबन्धों में जहाँ कहीं मौका मिला है, वहाँ प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। लेखक कहता है कि “इधर-उधर हरी-भरी लहलहाती, प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत उदारता के दर्शन कर सकते हैं।” शुक्ल जी ने पर्वत की ऊँची चोटियों की भव्यता का वर्णन किया है। साथ ही वायु से विलोड़ित जल प्रसार का भी आकाश के घने काले बादल, सान्ध्यकालीन लालिमा का सौन्दर्य, ग्रीष्म ऋतु से तिलमिलाती घरा, बिजली की कपने वाली कड़क आदि प्रकृति के विभिन्न रूप लेखक को अत्यधिक आकर्षित करते हैं।
रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा-शैली
शुक्ल जी की भाषा तत्सम् प्रधान परिनिष्ठित खड़ी बोली है। यह भाषा समीक्षा एवं आलोचना के लिए अत्यन्त सक्षम एवं समर्थ है। लेखक ने अपने सभी निबन्धों में अत्यन्त प्रौढ़ एवं प्रांजल हिन्दी भाषा का प्रयोग किया है। एक आलोचक के शब्दों में “शुक्ल जी की भाषा में विषयानुकूलता है, नवीन विषयों के प्रतिपादन की अद्भुत क्षमता है, भावानुकूलता है, साहित्यालोचन की विश्लेषणात्मक प्रणाली को अपनाकर गूढ़ से गूढ़ विषय के निरूपण की सतर्कता है, विज्ञान एवं दर्शन सम्बन्धी विषयों के निर्देशन एवं प्रतिपादन की पूर्णशक्ति है। शुक्ल जी की भाषा में जब कोई भी विचार आकर उपस्थित होता है, तब उनकी आन्तरिक एवं बाह्य अभिव्यंजना में एक विचित्र समन्वय दृष्टिगोचर होता है।”
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से शुक्ल जी ने उच्च कोटि के निबन्ध लिखे हैं। शुक्ल जी की भाषा का चमत्कार उन परिभाषाओं में देखा जा सकता है जो उन्होंने विविध मनोभावों के स्वरूप को प्रकट करने के लिए लिखे हैं। हास्य-व्यंग्य विनोद, गम्भीर विवेचनात्मक भावात्मक, आगमन, निगमन आदि सभी प्रकार की शैलियों का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है।
इन्हें भी पढ़े :-
हरिवंशराय बच्चन का जीवन परिचय
बालमुकुंद गुप्त का जीवन परिचय
मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय