Contents
फिराक गोरखपुरी जीवन परिचय
फिराक गोरखपुरी उर्दू, फारसी के महान शायर थे। उनका जन्म 28 अगस्त, 1896 ई० को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनका मूल नाम रघुपति सहाय फ़िराक था। उन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ई० में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए लेकिन स्वराज आंदोलन से प्रेरित होकर 1918 ई० में पद त्याग दिया।
1920 ई० में इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया जिसके कारण इन्हें डेढ़ वर्ष की जेल भी हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक के पद पर कार्य किया। उन्हें ‘गुले नगमा’ के लिए साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से अलंकृत किया गया। अंततः सन् 1983 ई० में ये अपनी महान शायरी, संसार को सौंप स्वर्ग सिधार गए।
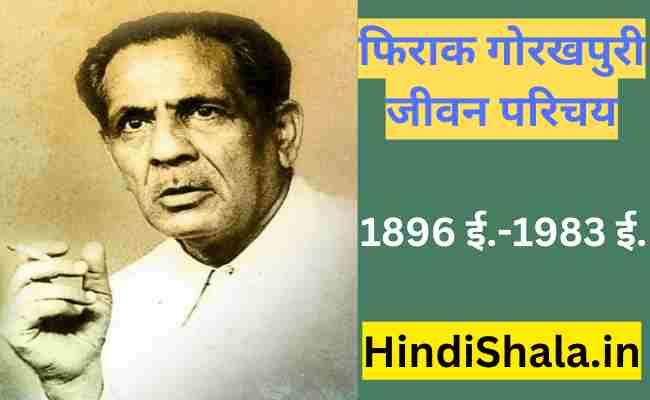
फिराक गोरखपुरी संक्षिप्त जीवनी
| नाम | रघुपति सहाय फ़िराक |
| जन्म | 28 अगस्त, 1896 ई. |
| जन्म स्थान | गोरखपुर, उत्तर प्रदेश |
| पिता का नाम | मुंशी गोरख प्रसाद |
| पत्नी का नाम | किशोरी देवी |
| निधन | 3 मार्च, 1982 |
| जीवंत आयु | 96 वर्ष |
प्रमुख रचनाएँ
गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए विषयों का पदार्पण कर प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ा। अनेक नए विषयों की खोज कर उन्होंने अनेक रुबाइयाँ, गजलें आदि लिखीं। इनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ निम्नलिखित हैं- गुले नगमा, बच्चें जिंदगी, रंग-ए-शायरी, उर्दू गजल गोई आदि।
साहित्यिक विशेषताएँ
फ़िराक गोरखपुरी उर्दू साहित्य के महान शायर माने जाते हैं। इनकी शायरी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
नवीन विषयों का चित्रण उर्दू शायरी का साहित्य रुमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। फिराक गोरखपुरी और नसीर आदि साहित्यकारों ने इस परंपरा को तोड़ा। फ़िराक ने परंपरागत भाव बोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नए विषयों से जोड़ा। उन्होंने उर्दू शायरी को रहस्य, रुमानियत और शास्त्रीयता से बाहर निकालकर सामाजिक दुःख-दर्द के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया।
वैयक्तिकता का चित्रण
फ़िराक गोरखपुरी ने उर्दू शायरी में व्यक्तिगत अनुभूति की ओर मोड़ा और उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से अपने सुख-दुःखों का चित्रण किया जैसे-
तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है।
सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके-चुपके रोते हैं।
शृंगार वर्णन
गोरखपुरी की शायरी में शृंगार रस का भी चित्रण हुआ है। इनकी शायरी में शृंगार के दोनों पक्षों के संयोग और वियोग का वर्णन मिलता है लेकिन संयोग की अपेक्षा विरहावस्था का अधिक चित्रण हुआ है। इनके साहित्य में एक प्रेमी-प्रेमिका वियोग की सजीव एवं मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है-
ऐसे में तू याद आये है अंजुमने भय में रिन्दों को।
रात गये गर्दा पै फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं।
वात्सल्य रस का चित्रण – गोरखपुरी की शायरी में वात्सल्य रस की अनुपम अभिव्यक्ति हुई है। वात्सल्य रस का चित्रण करते हुए ऐसा लगता है मानो कवि एक माँ का हृदय पा गए हों माँ का बच्चे के प्रति प्रेम तथा अपने नन्हें बच्चे को अपने आँचल से लगाकर माँ की अनुभूतियों का इन्होंने सजीव अंकन किया है। इन्होंने वात्सल्य रस की छोटी से छोटी अनुभूति का सजीव वर्णन किया है।
भारतीय संस्कृति का अनूठा चित्रण
फिराक गोरखपुरी एक सच्चे भारतीय थे। वे हिंदू-मुस्लिम आदि संकीर्णताओं से दूर एक मानव थे। इसीलिए उन्होंने कभी भी हिंदुओं धर्म के प्रति वैर भावना नहीं रखी बल्कि भारतीय संस्कृति, तीज त्योहार आदि का अनूठा चित्रण किया है। उनकी शायरी में हिंदू-मुसलमानों के अनेक त्योहारों की झांकी मिलती है। गोरखपुरी ने अपनी रुबाइयों में दीवाली, रक्षा बंधन आदि त्योहारों की सजीव अभिव्यक्ति की है।
देशभक्ति की भावना
फ़िराक गोरखपुरी एक सच्चे देशभक्त थे। सन् 1920 ई० में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण वे जेल भी गए थे। यही देशभक्ति की भावना उनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से भारतीय समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। (vii) प्रकृति चित्रण – गोरखपुरी जी प्रकृति से भी प्रेम करते थे जिसका परिणाम उनके अनूठे प्रकृति-सौंदर्य में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने साहित्य में वसंत ऋतु, बाग, उद्यान, टिमटिमाते तारे, फूलों की महक आदि का सजीव और मनोहारी चित्रण किया है।
भाषा शैली
गोरखपुरी जी उर्दू के श्रेष्ठ शायर हैं। उन्होंने अपनी शायरी को अभिव्यंजना प्रदान करने के लिए नई भाषा और नए शब्द भंडार का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, फ़ारसी, साधारण बोलचाल, खड़ी बोली हिंदी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। ये लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भी ‘मीर और गालिब’ की तरह कहने की शैली को साधकर साधारण मनुष्य से अपनी बात कही है।
इन्हें भी पढ़ें :-