Contents
काव्य लक्षण: काव्य वाङ्मय का प्राण है। इसलिए काव्य की उत्पत्ति के समय से ही उसके लक्षणों पर विचार होने लगा। काव्य क्या है ? इस मूलभूत प्रश्न की व्याख्या संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने- अपने दृष्टिकोण से की है। सर्वप्रथम संस्कृत विद्वानों द्वारा दी गई काव्य-परिभाषाओं को देखते है।
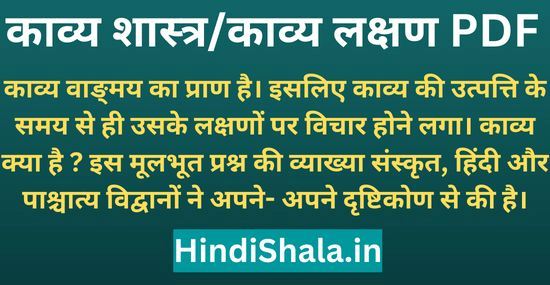
संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई काव्य-परिभाषाएँ
1. भरतमुनि:- आचार्य भरतमुनि ने ‘नाट्यशास्त्र’ में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है।
“मृदुललित पदाढ्यं गूढ़ं शब्दार्थहीनं,
जनपदसुखबोध्यं युक्तिमन्नृत्ययोज्यं।
बहुकृतरसमार्गं संधिसंधानयुक्तं,
स भवति शुभकाव्यं नाटकप्रेक्षकाणाम्॥”
अर्थात् जो कोमल और ललित पदों से युक्त, गूढ़ शब्द और अर्थ से विरहित, सर्वग्राहय, सबको सुख देने: वाला, नृत्य में प्रयुक्त किए जाने योग्य रस की विविध धाराएँ प्रवाहित करने वाला, संधियों के संधान से युक्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ काव्य कहा जाता है।
2. अग्निपुराण :- अग्निपुराण में शास्त्र, इतिहासादि से काव्य को भिन्न बतलाते हुए उसको इस प्रकार स्पष्ट किया है।
“संक्षेपाद् वाक्यमिष्टार्थव्यवचिछन्ना पदावली।
काव्यं स्फुरदलंकार गुणवद्दोषवर्जितम्।।”
अर्थात् जिसमें संक्षिप्त वाक्यों द्वारा अभीष्ट अर्थ की व्यंजना हो, अविच्छिन्न पदावली हो तथा जो अलंकार और काव्य-गुणों से युक्त तथा दोषों से रहित हो, उसी रचना को काव्य कहेंगे।
3. भामह :- आचार्य भामह ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ ‘काव्यालंकार’ में काव्य में शब्द और अर्थ की अवस्थिति को ही महत्त्व दिया है।
“शब्दार्थो सहितौ काव्यम्”
अर्थात् शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है।
4. दण्डी :- ‘दण्डी की काव्य- परिभाषा अग्निपुराण की काव्य परिभाषा से बहुत मिलती-जुलती है।
“शरीरं तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्नापदावली”
अर्थात् काव्य का शरीर वांछित अर्थ को उद्घाटित करनेवाली’ पदावली होती है।
5. वामन :- वामन ने काव्य लक्षण बतलाते समय अलंकारों को ही काव्य- सौंदर्य कहा है। इनके ‘काव्यालंकार सूत्र’ में दिए गए काव्य-संबंधी यह तीन सूत्र द्रष्टव्य हैं।
“काव्यं ग्राह्यमकरात्”
“सौन्दर्यमलंकार:”
“सदोषगुणालंकार- हानादाना भ्याम्”
अर्थात् अलंकार युक्त ही ग्राह्य होता है, सौंदर्य ही अलंकार है । काव्य और सौंदर्य काव्य के दोष रहित और गुण और अलंकार से युक्त होने पर ही निर्भर है। इससे स्पष्ट है कि वामन काव्य में गुण और अलंकार को आवश्यक मानते हैं।
यह भी पढ़े :- काव्य हेतु क्या होते है ?
6. रुद्रट :- रुद्रट ने एक प्रकार भामह की परिभाषा को दोहराते हुए कहा है।
“ननु शब्दार्थों काव्यं”
इसी प्रकार आचार्य रुद्रट ने भी भामह की भांति शब्द और अर्थ के समन्वय को ही काव्य माना है।
7. कुंतक :- आचार्य कुंतक वक्रोकितवादी थे, उन्होंने काव्य को वक्रोक्तिगर्भित शब्दार्थ कहा है।
“‘वक्रोक्ति काव्य-जीवितम्”
अर्थात् वक्रोक्ति सहित शब्द और अर्थ का साहित्य ही काव्य है।
8. मम्मट :- आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध लक्षण है, जो प्रौढ़ एवं सुदीर्घ चिंतन का परिणाम है।
“तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि”
अर्थात् शब्द और अर्थ का वह समन्वित रूप जो दोष रहित हो और गुण, अलंकार सहित हो तथा कहीं अलंकार स्पष्ट भी न हों, काव्य होता है।’
9. जयदेव :- मम्मट के बाद जयदेव का काव्य- लक्षण उल्लेखनीय है । नाट्यशास्त्र के समान जयदेव ने भी काव्य-लक्षण में लंबे-चौड़े शब्दों का प्रयोग किया है। ‘चंद्रालोक’ में वे लिखते हैं-
“निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुण भूषणा।सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक्काव्य नामवाक्”
अर्थात् वह वाणी जो दोष रहित हो, लक्षणों से युक्त हो, रीति और गुण से विभूषित हो, अलंकार और तथा वृत्तियों से विशिष्ट हो, काव्य की संज्ञा प्राप्त कर सकेगी । इस परिभाषा में जयदेव ने के सभी तत्त्वों का समावेश कर लिया है।
10. विश्वनाथ :- रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने ‘साहित्यदर्पण’ में रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है- –
“वाक्यं रसात्मकं काव्यं”
11. पंडित जगन्नाथ :- ‘रसगंगाधर’ नामक ग्रंथ में पंडितराज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है।
“रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्”
इस प्रकार संस्कृत आचार्यों ने काव्य के शरीर और आत्मा तथा उसकी विशेषताओं पर विशद वर्णन किया है।
हिंदी विद्वानों द्वारा दी गई काव्य परिभाषाएँ
हिंदी के प्राचीन आचार्यों ने काव्य-लक्षण देते समय प्रायः संस्कृत के आचार्यों के काव्य-लक्षणों का छायानुवाद-सा कर दिया है।
1. चिंतामणि त्रिपाठी के शब्दों में :-
“सगुन अलंकारन सहित दोषरहित जो होई
शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई”
“उपर्युक्त परिभाषा में स्पष्ट रूप से मम्मट की परिभाषा 4/7 पुनरुदरणी करने की चेष्टा की गई है। परंतु उसमें वह प्राणवला नहीं, जो आचार्य मम्मट की मूल परिभाषा में है। रीतिकाल के अन्य आचार्यों की परिभाषाएँ भी इसी प्रकार पिष्टपेषण मात्र हैं।
रीतियुग के कुछ प्रसिद्ध आचार्यों की काव्य-परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-
2. कुलपति द्वारा दी गई परिभाषा :-
“जग ते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित्र
यह लच्छन मैंने किया समझ ग्रंथ बहु चित्र”
3. देवकृत परिभाषा :-
“शब्द’ जीव तिहि अरथ मन रसमय सुजस सरीर
चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर”
4. श्रीपति द्वारा दी गई परिभाषा :-
“शब्द अर्थ बिन दोष गुन अलंकार रसवान
ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान”
5. आचार्य सोमनाथ की काव्य-परिभाषा :-
“सगुन पदारथ दोष दिनु पिंगल मत अविरुद्ध
भूषन जुत कति कर्म जो सो कवित कहि सुद्ध”
(6) भिखारीदास की परिभाषा :-
“व्यंग्य जीवन कहि कवित को, हृदय सुधुनि पहचानि
शब्द अर्थ कहि देह पुनि भूषण भूषण जानि”
आधुनिक विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य-लक्षण
आधुनिक युग के हिंदी विद्वानों में पं महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम अग्रगण्य हैं। उन्होंने ‘काव्य’ और कविता’ शीर्षक लेख में काव्य के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है।
“जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं, तब वही कविता कहलाने लगते हैं, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक !”
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ‘चिंतामणि’ में ‘कविता क्या है। शीर्षक लेख में काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है – “जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है | हृदय मुक्ता की इसी मुक्ति की साधना के लिए वाणी जो शब्द – विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।”
इस प्रकार शुक्ल जी ने काव्य में रंग क को महत्त्व दिया है। यह प्राचीन रसवादी आचार्यों के अनुयायी प्रतीत होते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ‘रसज्ञ रंजन’ में लिखा है – “शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परमावश्यक है। चमत्कार अलंकारमूलक हो सकता है, वह अभिव्यक्तिमूलक एवं औचित्यमूलक भी हो सकता है।”
जयशंकर प्रसाद जी काव्य अनुभूति मानते हैं। को आत्मा की मूल संकल्पात्मक अनुभूति मानते हैं।
अज्ञेय कहते है कि “कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है।”
धूमिल “कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है।”
आधुनिक युग की श्रेष्ठ कवयित्री महादेवी वर्मा ने भी काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला है – “कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएँ किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं।”
उपन्यास-सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी काव्य को जीवन की आलोचना मानते थे।
पाश्चात्य विद्वानों के मत
पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। वे अन्य कलाओं के सदृश कविता को भी अनुकृत मानते थे । एरिस्टाटिल ने उसे ‘छन्दोबद्ध अनुकृति’ कहकर ही परिभाषित किया है।
होरेस ने ‘आर्ट आफ पोयट्री’ नामक रचना में कवि कर्म को चित्रकार के कार्य के सदृश कहा है।
शेक्सपीयर ने Mid Summer Night’s Dream में कविता को कल्पना की दुहिता व्यंजित की है।
वईसवर्थ ने काव्य में कल्पना के स्थान पर भावना को महत्त्व दिया है। अर्थात् कविता उत्कट भावनाओं का सहज उद्रेक है। इनकी उत्पत्ति शांति में संचित अनुभूतियों से होती है।
मिल्टन ने काव्य में राग और वासनात्मक प्रवेश को महत्त्व दिया है। वह उसकी मसादात्मकता और सरलता में भी विश्वास करता है । ‘Essay On Education’ एक स्थल पर उसने लिखा है – “Poetry should be Simple, Sensuous & passionate!”
कॉलरिज काव्य में भावनाओं की क्रमिक अभिव्यक्ति को सुंदर शब्दों द्वारा सजाने के पक्ष में है “Poetry is the best words in the best order.”
ड्राइडेन ने कविता में संगीत तत्त्व को महत्त्व दिया है। उसके अनुसार कविता व्यक्त संगीत है – “Poetry is the articulate music.”
मैथ्यू आर्नल्ड काव्य में कल्पना के स्थान पर जीवन और विचारात्मक व्याख्या को महत्त्व दिया है – “Poetry is at bottom a criticism of life.”
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि काव्य के लक्षण के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं जिससे ‘काव्य’ क्या है ‘ प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हिंदी विषय के ऐसे ही शानदार आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आप हिंदीशाला को विजिट करते रहें।