Contents
- काव्य प्रयोजन की परिभाषा
- संस्कृत आचार्यों का मत
- 1. आचार्य भरतमुनि
- 2. आचार्य भामह के अनुसार
- 3. आचार्य मम्मट के अनुसार
- 4. आचार्य दंडी
- 5. आचार्य विश्वनाथ
- 6. रुद्रट
- 8. कुंतक
- हिंदी कवियों का मत
- 1. तुलसीदास
- 2. कबीरदास
- 3. सूरदास
- 4. भिखारी दास
- 5. कुलपति मिश्र
- 6. सोमनाथ
- 7. मैथिलीशरण गुप्त
- 8. डॉ नगेंद्र
- 9. महावीरप्रसाद द्विवेदी
- 10. महादेवी वर्मा
- 11. नंददुलारे वाजपेयी
- 12. हरिऔध
- 13. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
- 14. हजारीप्रसाद द्विवेदी
- 15. सुमित्रानन्दन पंत
- 16. डॉ गुलाबराय
- 17. प्रेमचंद
- पाश्चात्य चिंतकों के मत
आज के इस नए आर्टिकल में हम काव्य प्रयोजन को पढ़ने जा रहें है। हिंदी और संस्कृत के पाठकों के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हम काव्य प्रयोजन का अर्थ, काव्य प्रयोजन की परिभाषा एवं संस्कृत, हिंदी तथा पाश्चात्य चिंतकों द्वारा दिए गए मतों पर चर्चा करने जा रहें है। आप काव्य प्रयोजन के साथ-साथ काव्य लक्षण और काव्य हेतु को भी पढ़ सकते है।
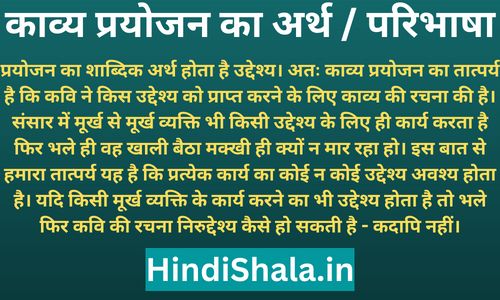
काव्य प्रयोजन की परिभाषा
“प्रयोजनं विना तु मन्दोऽपि न प्रवर्तते |”
संस्कृत आचार्यों का मत
1. आचार्य भरतमुनि
भरतमुनि ने अपने ग्रंथ ‘नाट्यशास्त्र’ में लिखा है –
“धर्मं यशस्यं आयुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम्।
लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति ।।”
अर्थात एक नाटक लेखन के निबंध 6 प्रयोजन माने जा सकते हैं –
1.धर्म
2.यस
3.आयु
4. हित
5.बुद्धि का विकास
6.लौकिक ज्ञान
अन्य स्थान पर वे लिखते हैं –
दु:खार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्वीनाम्।
विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति।।”
अर्थात् दु:खार्त , श्रमार्त एवं शोकार्त व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति ही काव्य लेखन का प्रयोजन है |
2. आचार्य भामह के अनुसार
भामह की रचना ‘काव्यालंकार’ के अनुसार काव्य प्रयोजन है –
“धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।
करोति कीर्तिं प्रीतिञ्च साधुकाव्य निबन्धनम्।।”
अलंकारवादी आचार्य भामह ने अपनी कृति ‘काव्यालंकार’ में काव्य प्रयोजन के संबंध में अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि काव्य की रचना धर्म, अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति तथा कलाओं में निपुणता प्राप्त करने के उद्देश्यों से की जाती है। इसके साथ ही साथ वह कृति और प्रीति प्रदान करने वाली भी होती है। भामह ने धर्म, धन, यश, काम, कृति और मोक्ष की प्राप्ति को ही काव्य का प्रयोजन बताया है।
3. आचार्य मम्मट के अनुसार
आचार्य मम्मट ने अपनी रचना ‘काव्यप्रकाश’ में काव्य प्रयोजनों को इस प्रकार व्यक्त किया है –
“काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परिनिर्वृत्त्ये कान्तासम्मितयोपदेशयुजे।।”
आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्यप्रकाश में काव्य प्रयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि सफल काव्य प्रयोजन जो संसार के सभी प्रयोजनों में मुख्य है तथा जिसके प्राप्त होते ही तुरंत आनंद का अनुभव होता है। उस आनंद के सामने शेष ज्ञान वस्तुओं का ज्ञान भी तिरोहित हो जाता है। वह प्रयोजन कवि और पाठक दोनों के लिए है।
मम्मट के अनुसार काव्य के छह प्रयोजन हैं , जो इस प्रकार हैं –
क.यश प्राप्ति – काव्य लेखन से कवि को यश प्राप्त होता है और वह सदा के लिए अमर हो जाता है |
ख.अर्थ प्राप्ति – काव्य लेखन से कवि को अर्थ अर्थात् धन की प्राप्ति होती है |
ग. लोक व्यवहार का ज्ञान – इसका संबंध पाठकों से है अर्थात् एक श्रेष्ठ काव्य के पठन से पाठकों को मानवोचित शिक्षा प्राप्त होती है |
घ. अनिष्ट का निवारण – यहाँ ‘शिवेतर’ का अर्थ है – अमंगल और ‘क्षतये’ का अर्थ है – विनाश अर्थात् काव्य लेखन से कवि के एवं काव्य के पठन से पाठक के अनिष्ट का निवारण होता है |
ङ. आत्म शांति – इसका संबंध मुख्यत: पाठक से है अर्थात् काव्य पठन से पाठक को पढ़ने के साथ ही आनंद का अनुभव होता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है |
च. कान्तासम्मित उपदेश – उपदेश तीन प्रकार के माने जाते हैं –
(i) प्रभु सम्मित उपदेश – ऐसा उपदेश जो हमारे लिए हितकर तो होता है ,परन्तु रुचिकर नहीं होता , वह प्रभु सम्मित उपदेश कहलाता है |
(ii) मित्र सम्मित उपदेश – यह उपदेश हितकर भी होता है और रुचिकर भी ,परन्तु इसकी अवहेलना भी की जा सकती है |
(iii) कान्तासम्मित उपदेश – यह उपदेश हितकर भी होता है और रुचिकर भी होता है तथा इसकी कभी अवहेलना भी नहीं की जा सकती है | काव्य का उपदेश इसी श्रेणी का उपदेश माना जाता है |
4. आचार्य दंडी
आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ “काव्यदर्श’ में प्रत्यक्ष रूप से तो काव्य प्रयोजन की चर्चा नहीं की, परंतु उन्होंने वाणी के लिए जो प्रयोजन बतलाए हैं उन्हें ही इस काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने वाणी की महत्ता का विवेचन करते हुए काव्य को तीनों लोकों में ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला कवि व काव्य को यश प्रदान करने वाला बताया है।
दंडी के इस कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञान व यश की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है। दंडी ने काव्य प्रयोजन के संबंध में सांसारिक व व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया है और उन्होंने इस संबंध में दार्शनिकता को नकारा है।
5. आचार्य विश्वनाथ
विश्वनाथ ने अपने ग्रन्थ ‘साहित्यदर्पण’ में काव्य प्रयोजनों का विवेचन इस प्रकार किया गया है –
“चतुर्वर्गफलप्राप्ति: सुखादल्पधियामपि।
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरुप्यते ।।”
6. रुद्रट
पुरुषार्थ-चतुष्ट्य, अनर्थ का शमन, विपत्ति-निवारण, रोग-मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति।
नौवीं शताब्दी के संस्कृत आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य के प्रयोजन पर अधिक विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने काव्य को अलंकारों में युक्त और दोषों के न होने को स्वीकार किया है।
इनके अनुसार काव्य के असंख्य प्रयोजन होते हैं। इस संबंध में वे स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार समुंदर में गिरी-मणियों को गिन पाना असंभव है वैसे ही काव्य प्रयोजनों का अनुमान लगाना भी कठिन है। काव्य की रचना करते समय कवि के समक्ष धन, यश, कृति आदि लक्ष्य होते है परंतु इनमें से यश ही सबसे बड़ा काव्य प्रयोजन है।
8. कुंतक
‘वक्रोक्तिजीवित’ के रचनाकार कुंतक में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों से थोड़ा हटकर काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। कुंतक कहते हैं कि अभिजात्य कुल उत्पन्न सहृदय के मन में आनंद उत्पन्न करने वाला और कोमल व मृदु शैली में लिखा गया धर्मादि सिद्धि का मार्ग ही काव्य है। कुंतक ने केवल सहृदय की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। वे परमानंद की प्राप्ति को ही काव्य प्रयोजन कहते हैं।
हिंदी कवियों का मत
1. तुलसीदास
तुलसीदास ने स्वान्त: सुखाय को साहित्य का उद्देश्य मानते हुए लिखा है –
“स्वान्त: सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति”
2. कबीरदास
’’तुम जिन जानौ गीत है यह निज ब्रह्म विचार।’’
3. सूरदास
सूरदास ने कृष्ण के ’सगुण-लीला पदों का गान’ ही अपनी काव्य रचना का प्रयोजन माना है।
4. भिखारी दास
इन्होंने यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हुए कहा है कि काव्य के पांच प्रयोजन होते हैं तपः, पुंज का फल, संपत्ति लोभ, यशप्राप्ति, सहृदयों को आनंद की उपलब्धि तथा सुखपूर्वक शिक्षा की प्राप्ति।
5. कुलपति मिश्र
आचार्य कुलपति मिश्र ने यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान को काव्य का प्रयोजन बताया है।
6. सोमनाथ
आचार्य सोमनाथ ने कीर्ति, धन, मनोरंजन, अनिष्टनाश और उपदेश को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है।
7. मैथिलीशरण गुप्त
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है।
केवल मनोरंजन ने कवि का क्रम होना चाहिए।
उसमें उचित उपदेश का भी मन होना चाहिए।
8. डॉ नगेंद्र
नगेंद्र की दृष्टि में काव्य के मूलतः दो प्रयोजन है – आनंद और लोकमंगल, जिनमें सापेक्षिक मूल्य आनंद का ही अधिक है।
9. महावीरप्रसाद द्विवेदी
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ’ज्ञान का विस्तार’ और ‘आनन्द की अनुभूति’ के रूप में काव्य का प्रयोजन बताया है।
10. महादेवी वर्मा
’मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना’।
11. नंददुलारे वाजपेयी
नंददुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य-प्रयोजन ’आत्मानुभूति’ होता है।
12. हरिऔध
हरिऔध के अनुसार काव्य-प्रयोजन ’आनन्दानुभूति’ होता है।
13. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ’आनन्द की अनुभूति’और ’लोकहित की भावना’ को प्रमुख काव्य-प्रयोजन माना है।
14. हजारीप्रसाद द्विवेदी
हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य-प्रयोजन ’मानव-कल्याण’ होता है।
15. सुमित्रानन्दन पंत
सुमित्रानन्दन पंत ने ’स्वान्तःसुखाय’ और ’लोकहिताय’ को काव्य-प्रयोजन माना है।
16. डॉ गुलाबराय
गुलाबराय के मत में रसानंद ही जीवन का रस है।
17. प्रेमचंद
प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना स्वीकार किया है।
पाश्चात्य चिंतकों के मत
1. सुकरात – इनके अनुसार दैवी प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है।
2. प्लेटो – प्लेटो लोकमंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं।
3. अरस्तु – इनके अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है। यह अनैतिक नहीं हो सकता।
4. होरेस – होरेस आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं।
5. मैथ्यू आर्नल्ड – इनके दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन है।