Contents
लॉजाइन्स के उदात्त की अवधारणा का विवेचन
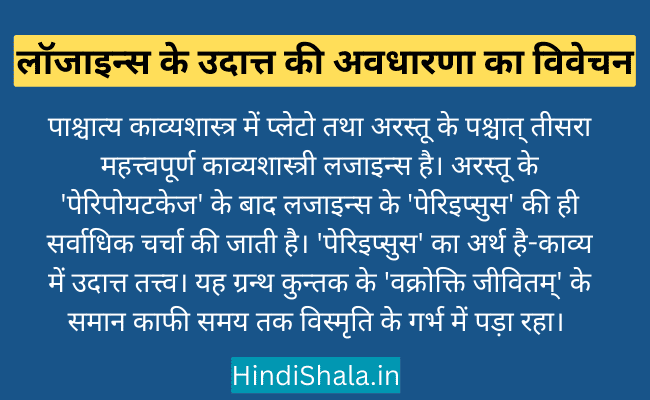
1. लॉज़ाइन्स का संक्षिप्त जीवन-वृत्त
पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो तथा अरस्तू के पश्चात् तीसरा महत्त्वपूर्ण काव्यशास्त्री लजाइन्स है। अरस्तू के ‘पेरिपोयटकेज’ के बाद लजाइन्स के ‘पेरिइप्सुस’ की ही सर्वाधिक चर्चा की जाती है। ‘पेरिइप्सुस’ का अर्थ है-काव्य में उदात्त तत्त्व। यह ग्रन्थ कुन्तक के ‘वक्रोक्ति जीवितम्’ के समान काफी समय तक विस्मृति के गर्भ में पड़ा रहा। 1554 ई. में इस ग्रन्थ की पूर्ण प्रति उपलब्ध हो सकी। इस ग्रन्थ के रचयिता लजाइन्स को लेकर भी विद्वानों में काफी विवाद चलता रहा। कुछ आलोचकों ने पेरिइप्सुस लेखक जेनोबिया के मन्त्री लॉजाइन्स को माना है जो कि एक सुप्रसिद्ध वीर था। इसका समय तीसरी शताब्दी है। इसने पलमीरा की महारानी जेनोबिया की बड़ी निष्ठा से सेवा की थी। ‘स्कॉट जेम्स’ ने इसका समर्थन किया है। आरम्भ में पेरिइप्स का अशुद्ध अनुवाद किया गया- On the sublime.
2. पेरिइप्सुस का कथ्य
लीजाइन्स की यह कृति केवल 60 पृष्ठों में प्रकाशित हुई है। लेकिन इसके छोटे-छोटे की संख्या 44 है। यह रचना पत्र शैली में ‘रोमी’ मित्र को सम्बोधित की गई है। इसका केवल दो-तिहाई राहत उपलब्ध है। इसके कथ्य (प्रतिपाय) को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। आरम्भ में On the Sublime हो आधार मानकर यह कहा गया था कि इस का प्रतिपाय उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं और धारणाओं विश्लेषण है। लेकिन डॉ. नगेन्द्र ने स्वीकार किया है इसमें उदात्त शैली के आधार तत्त्वों का विवेचन ही प्रधान ” एटाकैन्स ने भी लिखा है-
“What he has in mind is rather elevation, all that raises a style above ordinary and gives to distinction in its widest and truest sense.”
3. काव्य सम्बन्धी धारणाएँ
लॉज़ाइन्स पूर्व यह धारणा थी कि कवि का मुख्य कर्म पाठक या प्रेक्षक को शिक्षा देना और आनन्द प्रदान करना है। बाद में अलंकारवादियों ने संतुलित भाषा और सुव्यवस्थित तर्क पर बल दिया ताकि पाठक लेखक की बात को स्वीकार कर ले अर्थात् काव्य का लक्ष्य बन गया-शिक्षा देना, आनन्द प्रदान करना और अपनी बात को मनवाना। उदाहरण के रूप में होमर काव्य की सफलता श्रोताओं को मुग्ध करने में मानता था।
अरिस्टोफेनिस कविता का उद्देश्य पाठकों को सुधारना मानता था। लॉज़ाइन्स ने अनुभव किया काव्य में इन तीनों यातों-शिक्षा देना, आनन्द प्रदान करना और अपनी बात मनवाना से कुछ अधिक है। उसने एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रस्तुत किया- “काव्य या साहित्य का चरम उद्देश्य चरमोल्लास प्रदान करना है तथा पाठक या श्रोता को बेयान्तर शून्य बनाना है।”
यही नहीं, लीज़ाइन्स ने कवि के अध्ययन और अभ्यास पर भी बल दिया। वह स्वयं एक कुशल अलंकारशास्त्री था। उदात्त के स्रोतों की चर्चा करते हुए उसने उपाय के बहिरंग पक्ष पर भी समुचित प्रकाश डाला। अलंकारों के प्रयोग के बारे में उसने अपना मौलिक दृष्टिकोण व्यक्त किया।
यद्यपि उसने ‘कल्पना’ शब्द का प्रयोग तो नहीं किया लेकिन उसने यह भी कहा कि साहित्य का सम्बन्ध तर्क से नहीं है। साहित्य कल्पना द्वारा ही पाठकों को प्रभावित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉजाइन्स के काव्य में स्वच्छन्दतावादी तथा अभिजात्यवादी दोनों प्रकार के तत्त्व देखे जा सकते हैं। वे निश्चय से एक सन्तुलित विचारों वाले समन्वयवादी आलोचक एवं विचारक थे। स्कॉट जेम्स ने तो उसको प्रथम स्वच्छन्दतावादी आलोचक स्वीकार किया है। वे लिखते हैं-
“Though he was the first to expound doctrines upon which romanticism rests he tumed and tempered them with what is sanest in classicism.”
4. उदात्त का स्वरूप
लजाइन्स ने अपने मन्तव्य को कैकिलियस द्वारा प्रतिपादित उदात्त (sublime) का सुधार बताया है। सम्पूर्ण विषय की गरिमा को देखते हुए कैकिलियत का उदात्त सम्बन्धी प्रतिपादन बहुत निम्न स्तर का था। यह लजाइन्स की उदारता का प्रमाण है कि उसने अपने पूर्ववर्ती कंकिलियस को उदात्त का प्रतिपादन करने का गौरव प्रदान किया। लॉज़ाइन्स ने अपनी रचना पेरिइप्सुस में उदात्त की सविस्तार व्याख्या की है। लजाइन्स ने उदात्त की कहीं पर भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। सम्भवतः उसके समय ‘उदात्त’ की परिभाषा विद्वानों को ज्ञात होगी, यही सोच कर उसने इसकी विस्तारपूर्वक परिभाषा नहीं दी।
लॉज़ाइम्स ने उदात्त क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह उचित समझा कि उदात्त क्या नहीं है, इस पर विचार किया जाए। ‘बोइलो’ नामक प्रसिद्ध पाश्चात्य आलोचक ने यह स्पष्ट किया कि लीज़ाइन्स का उदात्त निश्चित रूप से उदात्त शैली का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
शैली में भाषा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। जबकि उदात्त का संबंध भावगत और विचारगत उदारता से होता है। लॉजाइन्स की दृष्टि में उदात्त केवल भाषा के चमत्कार की क्षमता का ही परिचायक नहीं है, क्योंकि भाषा के साथ उदात्त का कोई मूल संबंध नहीं। उदात्त का मूल भाव तो मनुष्यगत या विचारगत जगत है। बोइलो ने जो इप्स का अर्थ सबलाईम किया या उससे एक नया विवाद खड़ा हो गया क्योंकि इप्सुम तो एक व्यापक अवधारणा है जबकि सबलाईम सीमित अवधारणा है। उदान की व्यापकता सक्लाईम में नहीं समा सकती। स्वयं लजाइन्स ने उदात्त के बारे में लिखा है-
“वह वाणी का ऐसा वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्य है जिससे महान कवियों और इतिहासकारों को जीवन में प्रतिष्ठा और यश मिला है।”
इस कथन के आधार पर ही उदात्त को समझा जा सकता है। वे कहते हैं-‘अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष का नाम उदास है’ (Sublimity is always an excellence in composition.) लीजाइन्स ने भावोत्कर्ष को काव्य का मूल तत्व माना। परन्तु भावोत्कर्ष या चरमोत्कर्ष की व्याख्या को नहीं बताया। परन्तु यह अवश्य स्वीकार किया कि काव्य का लक्ष्य चरमोल्लास प्रदान करना है अथवा श्रोता को वैद्यांतर-शून्य बनाना है।
इन्हें भी पढ़े :-
अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत
प्लेटो की काव्य संबंधी अवधारणा
भव्य कविता वही है जो आनन्दातिरेक के कारण हमें इतना निमग्न या तन्मय कर दे कि हम अपना मान भूल जाएँ और ऐसी भाव भूमि पर पहुँच जाएँ जहाँ निरी बौद्धिकता पंगु हो जाए। उपर्युक्त कथनों से मरना होता है कि लौंजाइन्स ने व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों आधारों पर उदात का विशलेषण किया। उन्हरि उदात्त के पाँच तत्त्व गिनवाए हैं—इनमें से कुछ का संबंध तो अंतरंग से है और कुछ का बहिरंग से है।
(क) अंतरंग पक्ष
(i) महान धारणाओं की क्षमता या विषय की गरिमा
(ii) उद्दाम और प्रेरणा उद्वेग या भावावेश की तीव्रता।
(ख) बहिरंग पक्ष
(i) समुचित अलंकार योजना
(ii) उत्कृष्ट भाषा
(iii) गरिमामय रचना विधान।
(क) अंतरंग पक्ष-
(i) महान धारणाओं की क्षमता
लौंजाइन्स के अनुसार उस कवि की रचना महान् हो सकती है जिसमें महान् धारणाओं की क्षमता है। कवि को महान बनाने के लिए अपनी आत्मा में उदान विचारों का पोषण करना होगा। यहाँ लॉजाइन्स का मतलब यह था कि कवि की कल्पना में उच्चता और विराटता होनी चाहिए। यह विराटता ही मनुष्य को क्षुद्रता से ऊपर उठाती है। जो व्यक्ति छोटे-छोटे विचारों और स्वायों से घिरा रहता है वह किसी महान् कृति की रचना नहीं कर सकता। इस बारे में डॉ. नगेन्द्र कहते भी हैं-
“यह संभव नहीं है कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्यों और विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य और अमर रचना कर सके। महानू शब्द उसी के मुख से निःसृत होते हैं जिनके विचार गंभीर और महान् हो ।”
जहाँ तक विषय की गरिमा का प्रश्न है तो उनका विचार था कि उदात्त की उत्पत्ति के लिए विषय केवल साधन है। महान् विषय एक साधन रूप में रचना को उदात्त रूप देता है। महान् कवियों की महान रचनाओं में महान विषयों की उद्भावना रहती है। महान विषय के लिए जन्मजात प्रतिभा तो आवश्यक है ही, इसके साथ-साथ कवि को महान कवियों की अमर रचनाओं को भी पढ़ना चाहिए। उनका विचार था कि महान् रचनाओं को पढ़ने से रचनाकार को नए संस्कार, नई विचार-शक्ति, नए भाव और एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है।
लजाइन्स उदात्त विचारों के लिए कल्पना और महान काव्य के अनुशीलन को तो आवश्यक मानते थे। साथ ही विशुद्ध विम्बों की योजना पर भी बल देते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि, ‘विषय अनन्त विस्तार वाता हो (सागर के समान) उसमें असाधारण शक्ति और उद्वेग हो (ज्वालामुखी के समान) तथा उसमें अलौकिक ऐश्वर्य और प्रभाव क्षमता हो (ईश्वर के समान) ।’ इन उदाहरणों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि लजाइन्स मानव मन की विराटता पर बल देता है। मानव मन की विराटता ही गरिमामयी विषय पर उदात्त काव्य रचना कर सकती है।
(ii)उद्दाम और प्रेरणा
प्रसूत उवेगलाइन्स ने प्रेरणा प्रसूत उद्वेग को उदात्त का दूसरा आन्तरिक तत्त्व माना है। भव्य आवेग से उनका मतलब था ऐसा आवेग जिससे हमारी आत्मा अपने आप ऊपर उठकर गर्व के ऊंचे आकाश में विचरण करने लगे तथा हर्ष और उल्लास से भर जाए। उन्होंने आवेग की दो कोटिया बताई हैं-भव्य और निम्न।
निम्न आवेग में वे उन आवेगों की चर्चा करते हैं जिनका संबंध दया, शोक, भय आदि से है। भव्य जावेग से आत्मा का उत्कर्ष होता है और निम्न आवेग से अपकर्ष होता है। उदात्त के लिए भव्य आवेग जरूरी है। वे कहते हैं-“मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ जो आवेग उन्मद् उत्साह के उद्दाम वेग से फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विशेष से पूर्ण कर देता है उसके यथास्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा उदात्त आता है वह अन्यत्र दुर्लभ है।” इसका मतलब है कि लींज़ाइन्स ने भव्य आवेग को आवश्यक माना है। वे उसी को उदात्त मानते हैं जो अपनी ऊर्जा-उल्लास आदि के समन्वित प्रभाव से ऐसी अनुभूति को जन्म देता है जो पाठक की सम्पूर्ण चेतना को अभिभूत कर देता है।
(ख) बहिरंग पक्ष-
(i) समुचित अलंकार योजना
लीजाइन्स ने अलंकारों के बारे में बहुत ही तर्कपूर्ण और मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। लॉज़ाइन्स से पहले अलंकारों के प्रयोग में मनोवैज्ञानिकता नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनके विचारानुसार अलंकार प्रयोग तभी सार्थक है यदि उनके प्रयोग से भावोत्कर्ष होता हो, आनन्द की प्राप्ति होती हो तथा सहृदय भाव विभोर हो उठता हो। पुनः सोजाइन्स ने यह स्वीकार किया कि अलंकार भावोत्कर्ष का साध्य नहीं, अपितु साधन है।
अलंकारों का प्रयोग सहज और स्वाभाविक होना चाहिए ताकि पाठक को यह पता ही न चले कि उसमें कोई अलंकार है। वस्तुतः अलंकार प्रयोग के बारे में लींज़ाइन्स की अवधारणा सर्वथा नवीन एवं मौलिकता है। इस दृष्टि से वे एक क्रान्तिकारी आलोचक प्रतीत होते हैं। उन्होंने केवल उन्हीं अलंकारों का विवेचन किया जो काव्य शैली को उत्कर्ष प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने निम्नलिखित अलंकारों का निर्देश दिया जो उदात्त के पोषक हैं-विस्तारणा, शपयोक्ति, प्रश्नालंकार, पिय व्यतिक्रम, पुनरावृत्ति, छिन्नवाक्य, प्रत्यक्षीकरण, संघपन, सार, रूप परिवर्तन, पर्यायोक्त रूपक तथा अतिशयोक्ति।
इस प्रकार लींज़ाइन्स ने यह वकालत की कि अलंकारों का प्रयोग बड़े ही संयम और विवेकपूर्ण के साथ होना चाहिए। अलंकारों का प्रयोग करते समय स्थान, रीति और अभिप्राय का ध्यान होना चाहिए।
(ii) उत्कृष्ट भाषा
भाषा भावों की वाहिका एवं अमूर्त काव्य का मूर्त रूप है। इसके परिवेश की उत्कृष्टता एवं समृद्धि में ही औदात्य का प्रकट रूप निहित है। भाषा का औदात्य कवि के महान् व्यक्तित्व का द्योतक होने के साथ-साथ कृति के अमरत्व का भी कारण है। शब्दों का सुनिश्चित चयन, उनका उपयुक्त ग्रंथन एवं उनका यथात्थान एवं यथासमय औचित्यपूर्ण प्रयोग निश्चय ही शैली को गरिमा प्रदान करता है। भाषा की सज्जा एवं समृद्धि उसके द्वारा प्रस्फुटित होने वाली भाव-राशि के दुर्निवार प्रभाव की उत्कृष्टता में योग देती है।
एक स्थान पर लॉज़ाइन्स ने लिखा है-
“औदात्य अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कृष्टता का नाम है।”
इस कथन से भाषा के महत्त्व एवं उसके प्रयोग की गरिमा स्पष्ट होती है। इससे आगे यह मान लेना कि लीजाइन्स का प्रतिपाद्य यही है, अधिक औचित्यपूर्ण नहीं जचता। शब्दों का सौन्दर्य कृति में आलोक विकीर्ण करता हुआ उसके महत्त्व एवं गरिमा का उद्घाटन करता है। “सुन्दर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं।” विचारों की महानता अथवा जावेगों की प्रचुरता औदात्य सृष्टि में पर्याप्त नहीं, उसे साधारणीकरण की स्थिति देने के लिए सुनियोजित शब्द योजना भी आवश्यक है।
उक्ति के औदात्य एवं भावावेग के प्राचुर्य का साधन भाषा ही है। कल्पना के उर्वर स्रोत की उपयुक्त वाहिका शब्दों के सुनियोजित विधान की प्रक्रिया ही है। जहाँ शब्दों का लावण्यमय गुम्फन विचारों एवं भावनाओं के ओज का प्रमुख वाहक होता है, वहाँ उनकी छिन्नता- भिन्नता औदात्य की बाधक बन बैठती है। अतः लेखक को बड़ी सावधानी से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
सुगठित भाषा का प्रभाव सहृदय के चित्त पर उसकी सारी असावधानता को अपने में निहित भाव-राशि की ओर केंद्रीभूत करने में निहित है। लौंजाइन्स के शब्दों में- “उदात्त भाषा का प्रभाव श्रोता के मन पर प्रत्यय के रूप में नहीं, वरन् भावोद्रेक के रूप में पड़ता है।” उदात्त भाषा में स्थान, ढंग, परिस्थिति एवं उद्देश्य के समन्वय एवं संगठन का भाव अन्तर्निहित है। कल्पना विलास की मनोरमता के लिये भाषा की कोमलता और चारुता ही वांछनीय है।
(iii) गरिमामयी रचना विधान
लीजाइन्स ने इस बात पर बल दिया कि काव्य का रचना विधान गरिमामय होना चाहिए, क्योंकि काव्य रचना के शब्द श्रोता के केवल कानों का ही स्पर्श नहीं करते बल्कि उसके भीतर गहरे उतर जाते हैं। अतः काव्यकृति में प्रयुक्त शब्दों में सामंजस्य होना चाहिए। इसके लिए लौजाइन्स ने रचना विधान के अन्तर्गत शब्दों, विचारों और कार्यों के अनेक रूपों के गुम्फन पर बल दिया है।
उनकी दृष्टि में वही सामंजस्य काव्य रचना का प्राण तत्त्व होता है और यह उदात्त शैली के लिए अनिवार्य है। इस संबंध में उन्होंने मानव की शरीर रचना का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अवयवों का अलग-अलग कोई महत्त्व नहीं है और ये सब मिलकर ही एक समग्र और सम्पूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं इसी प्रकार उदात्त शैली के सभी तत्त्व एकान्वित होने चाहिए।
इस संबंध में वे कहते हैं-
“बही काव्य-सृष्टि उत्कृष्ट है, जो पाठकों को एक बार नहीं वरन् बार-बार उत्तेजित और उद्वेलित कर सके, जो विभिन्न पेश, आकांक्षाओं, युगों और भाषाओं में मनुष्यों के सम्मुख बार-बार पढ़ी जाने पर उन्हें प्रभावित कर सके।”
गरिमामयी रचना विधान के लिए यद्यपि उन्होंने सामंजस्य की बार-बार चर्चा की है। इस सामंजस्य में भी वे संयम और सन्तुलन की बात कहते हैं। उनका विचार था कि अगर सामंजस्य हो तो वह सहज रूप में लाया जाए, ठूसा हुआ न हो। जब कोई कवि सामंजस्य बैठाने के लिए अनावश्यक प्रयत्न करता है तो सहजता का नाश हो जाता है। “ऐसा सामंजस्य ऊपर से सुन्दर अवश्य लगता है पर उसमें गंभीरता नहीं रहती, वह बनावटी हो जाता है। सामंजस्य का रूप ही हमारा ध्यान आकर्षित करता है, केवल शब्दार्य नहीं।”
6. कल्पना तत्त्व का समावेश
लॉज़ाइन्स ने स्पष्ट रूप से कल्पना तत्त्व की चर्चा नहीं की। बिम्बों का वर्णन करते समय वे निर्माण करने वाली शक्ति के रूप में कल्पना की चर्चा करते हैं। बिम्ब से उनका मतलब कल्पना चित्र है और उसकी प्रेरणा शक्ति के रूप में वे कल्पना को मानते हैं। उनके अनुसार कल्पना वह शक्ति। है जो पहले कवि को मानसिक रूप में वर्ण्य विषय का साक्षात्कार कराती है और फिर जिसकी सहायता से कवि भाषा में चित्रात्मकता द्वारा वर्ण्य विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वह पाठक के सामने सजीव हो उठता है। इस प्रकार लजाइन्स के कल्पना संबंधी विचार आज के कल्पना संबंधी विचारों से मेल खाते हैं।
7 . उदात्त के विरोधी तत्त्व (अवरोधक तत्त्व)
लौजाइन्स ने कुछ ऐसे अवरोधक तत्त्वों का भी वर्णन किया है जो विषय को स्पष्ट बनाने के मार्ग में बाधा का काम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने शब्दाडम्बर की चर्चा की है। इसे वह Tumidity या Bombast of Language कहते हैं। शब्दाडम्बर के प्रयोग से कवि और पाठक के बीच साधारणीकरण नहीं हो पाता। क्लिष्ट और दुरूह शब्दों के कारण कविता का आशय दब जाता है।
चंचल पद गुम्फन, असंयत वागू-विस्तार, हीन और क्षुद्र शब्दों वाले अर्थों का प्रयोग सभी उदात्त शैली को नष्ट कर देते हैं। पुनः लजाइन्स ने बाल्यता अर्थात बचकानेपन की भी चर्चा की है। इस प्रकार के बेतुके और मनमाने काल्पनिक प्रयोगों से काव्य कृति की महत्ता खत्म हो जाती है। उदाहरण के रूप में गीध को जीवित समाधि कहना वाक् स्फीति ही कही जाएगी। इसके बाद उन्होंने भावाडम्बर की चर्चा भी की है। यह भी एक प्रकार से उदात शैली का जघन्य दोष है भावों की अभिव्यक्ति मनमाने ढंग से करने से भावों की उदातत्ता नष्ट हो जाती है।
भले ही मानवीय भाव बड़े पावन होते हैं लेकिन उनमें कुछ नियम और सिद्धान्त जरूरी हैं। वे कहते हैं-“भावाडम्बर दोष वहाँ होता है जहाँ संयम के स्थान पर असंयम और खोखले आवेग का प्रदर्शन होता है। यह आवेग प्रकृति जन्य न होकर वैयक्तिक और थका देने वाला होता है।” पुनः लजाइन्स ने नवीनता की खोज के लिए आडम्बर का विरोध किया है। कुछ कवि नवीनता की खोज के चक्कर में ऊल-जलूल कल्पनाएँ करते. हैं और अस्पष्टत शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अभिव्यजंना की क्षुद्रता, अत्यन्त संक्षिप्तता, अनावश्यक साजसज्जा, संगीत और लय का आधिक्य आदि भी उदात्त के विरोधी तत्त्व हैं।
8 . लौजाइन्स की देन
लीज़ाइन्स ने अपने पूर्ववर्ती आलोचकों की तुलना में प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए। प्लेटो के प्रभाव के कारण उन्होंने कवि के उत्कृष्ट व्यक्तित्व को आवश्यक माना। साथ ही अरस्तू से प्रभावित होकर उन्होंने काव्य शरीर के गठन पर बल दिया। लेकिन काव्य में भावात्मक उत्तेजना पर बल देना उनके मौलिक चिन्तन का परिणाम है। उन्होंने काव्य के सौन्दर्य को शास्त्र कसौटी पर कसा। जहाँ तक उनकी महान धारणा के सिद्धान्त का प्रश्न है, यह उनकी मौलिक देन कही जा सकती है। इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर ड्राइडन, एडीसन तथा वर्ड्सवर्थ जैसे महान् कवियों और आलोचकों को प्रभावित किया।
वस्तुतः आज काव्य आलोचना संबंधी जितनी भी धारणाएँ हैं, उन सबमें लौंजाइन्स का प्रभाव देखा जा सकता है। भावोत्कटता, लौकिकता, ऐश्वर्य तथा उत्कट प्रभाव क्षमता आदि गुणों का उल्लेख जो उन्होंने किया, परवर्ती कवियों ने भी उन्हें स्वीकार किया। लौजाइन्स का ग्रंथ ‘पेरिइप्सुस’ साहित्य के मूल प्रश्नों पर विचार करता है और उसके शाश्वत् सिद्धान्तों का उल्लेख करता है। उसकी सबसे बड़ी देन है कि उसने सदोष महान् कृति को निर्दोष साधारण कृति से ऊँचा माना है, क्योंकि महान रचना में ही दोषों की संभावना हो सकती है। वे कहते भी हैं-
“Great flights are necessity involve great risks from which pedestrian creatures are free”.
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लॉज़ाइन्स ने पेरिइप्सस में उदात्त की समुचित और सारगर्भित व्याख्या की है। पाश्वात्य काव्य परम्परा में लौंजाइन्स का मत आज भी विशेष स्थान रखता है।